अतीत का आईना
त्रिलोक दीप की कलम से
1969 में पहली बार लद्दाख गया था फौजियों के साथ। रास्ते में मुझे दो जानकारियां ऐसी मिलीं जो उस समय मेरे लिए नई थीं। एक, द्रास दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा स्थान है और दूसरी लद्दाख में एक ऐसा यूरोपीय विद्वान अपना पूर्व निश्चित रास्ता न पाकर लद्दाख पहुंच गया और यहां तिब्बती भाषा के शब्दकोश और व्याकरण को लिखने में ऐसा जुटा कि उसे अपना मूल लक्ष्य बिसर गया। मैंने उसी वक़्त मन ही मन अपने से दो वादे किये। एक, दुनिया का सब से ठंडा स्थान देखने का और दूसरे उस यूरोपीय जिज्ञासु विद्वान की तपोभूमि के साथ साथ उनसे जुड़े कुछ इलाकों को देखने का भी जहां का रास्ता उसने ज़्यादातर पैदल चल कर तय किया था। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान साइबेरिया जाने का अवसर मुझे 1987 में प्राप्त हुआ था। अपने फेसबुक के मित्रों से अपनी साइबेरिया यात्रा मैं पहले ही शेयर कर चुका हूं।
अब बात करते हैं अपने आपसे किए गए दूसरे वादे की। उस यूरोपीय विद्वान के बारे में कुछ जानकारियां लद्दाख में मिलीं, कुछ शिमला में, कुछ लाहौर में, कुछ कलकत्ता (आज का कोलकाता) और अंत में दार्जीलिंग में। मुझे हंगरी जाने के तीन अवसर मिले। एक अवसर पर राजधानी बुदापेश्त में मेरा उस समय का साथी पीटर अकादेमी ऑफ साइंसेस दिखाने ले गया। उस भवन के बाहर लगी मूर्ति को देखकर मेरे मुंह से सहसा निकल गया कि ‘यह तो चोमा की मूर्ति है। ‘ अब उसके चौंकने की बारी थी। बोला, सर अभी हम अकादेमी के भीतर गये नहीं और आपने उस व्यक्ति की मूर्ति पहचान ली जिस के विषय में बताने के लिए मैं आपको यहां लाया हूं। उसकी समस्या का समाधान करते हुए मैंने उसे बताया कि चोमा की एक मूर्ति दार्जीलिंग में भी है । जी हां , मैं जिस यूरोपीय विद्वान का ज़िक्र कर रहा था उसका नाम है अलेक्जांडर चोमा दे कोरोश जिन्हें हंगरी में कोरोशी चोमा शानदौर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली से रवाना होने से पहले उस समय के हंगरी के सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक योसेफ साबो ने मुझे बताया था कि’चोमा भारत में हंगरी की सांस्कृतिक धुरी हैं और उनकी खोजी और जिज्ञासु सोच ने दोनों देशों को निकट लाने में अहम भूमिका निभाई है। यही कारण है कि भारत आने वाला हरकोई हंगेरी दार्जीलिंग की यात्रा के बिना अपने सफर को अधूरा मानता है। हमारे लिए दार्जीलिंग पुण्य भूमि है जहां चोमा के रूप में हमारे देश की रूह दफन है और उन्हें श्रद्धांजलि देना हमारा पुनीत कर्त्तव्य।’
कभी कभी कुछ लोग अनोखे अंदाज में यह भी कहते पाये जाते हैं कि चोमा चले तो थे अपने देश की उत्पत्ति, उद्भव का स्रोत या कह सकते हैं अपने देश का कुल देवता ढूंढ़ने लेकिन भटक कोलंबस की तरह गये। जैसे कोलंबस निकले थे हिंदुस्तान की खोज में लेकिन खोज डाला उन्होंने अमेरिका। परन्तु चोमा के साथ ऐसी तुलना न तो रुचती है और न ही सटीक बैठती है। हंगरी की अकादेमी में एक चोमा कक्ष है जहां चोमा से जुड़ा साहित्य, उनकी पांडुलिपियां, उनके एकत्र किये अनेक दस्तावेज, जगह जगह उनकी पहनी गयीं पोशाकें आदि शामिल हैं। बताया गया कि चोमा ऐसी विलक्षण बुद्धि का छात्र था जिस के ज़ेहन में स्कूल के दिनों से ही एक ख्वाब सा ही आना शुरू हो गया था कि क्यों न हम अपने देश के अस्तित्व और उसके मूल के बारे में जानने की कोशिश करें। कोई कहता हम लोग हूण हैं तो कोई हमें मंगोल बताते हुए मध्य एशिया का कहते। चोमा के दो और सहपाठी भी इस सपने को साकार होते देखने की गर्ज़ से उसके हो लिये। वह यह भी जानना चाहते थे कि अगर यह सच है तो हम यूरोप से कैसे जुड़े। उम्र बढ़ने के साथ चोमा का सपना तो उनके साथ जवान होता चला गया लेकिन उनके दूसरे दो साथियों के लिए वह स्कूली खेल से ज़्यादा कुछ नहीं था। हंगरी के ट्रांसिलवनिया के कोरोश में अप्रैल 1784 में चोमा का जन्म एक गरीब घर में हुआ जो सैकड़ों वर्षों से सैनिक जागीरदारों से जुड़ा था और राष्ट्रभक्तों का परिवार माना जाता था। छुटपन से ही पढ़ाकू और जिज्ञासु प्रवृति का होने से चोमा का ध्यान शस्त्रों के बजाय शास्त्रों में रमा रहता। उन्हें लोग बेचैन रूह और तबियत का इंसान मानते थे। चोमा के एक अध्यापक थे प्रोफेसर सैमुएल हेंगेदुश जो उनकी रुचियों और दृढ़ विचारधारा से परिचित थे। उनकी कोशिशों से चोमा ने जर्मनी के गोटिंगें विश्वविद्यालय में लंबे समय तक अध्ययन किया औऱ इतिहास और प्राच्य विद्या के विद्वान बन गये।उन्होंने ने लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेज़ी आदि भाषाओं का ज्ञान भी अर्जित किया। विदेश में गहन अध्ययन करने के बाद जब चोमा स्वदेश लौटे तो कई नौकरियां उनका इंतजार कर रही थीं। उनके प्रोफेसर हेंगेदुश अब उनके जिगरी दोस्त बन चुके थे। जब चोमा से नौकरी का उल्लेख हुआ तो उन्होंने साफ बता दिया कि पहले वह स्लोवेनिक भाषा सीखेंगे और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करेंगे, अपने अतीत की खोज की यात्रा। चोमा ने मध्य एशिया और वह भी अकेले तथा पैदल यात्रा का उनको फैसला सुना कर एकबारगी हिला दिया। इसपर चोमा ने हंसते हुए अपने प्रोफेसर बनाम दोस्त हेंगेदुश को उत्तर दिया, ‘यही तो ज़िंदगी है भाई। ‘हेंगेदुश का चोमा से इतना लगाव था कि वह उसकी हर गतिविधि और आगे के कदम से वाकिफ रहा करते थे। प्रोफेसर हेंगेदुश ने अपने एक संस्मरण में लिखा है कि चोमा एक दिन आये और बोले ‘मैं कल से अपनी यात्रा पर निकलने वाला हूं।’ उनकी आंखों में एक अजब विश्वास भरी चमक थी और लगता था कि उनकी आत्मा कुछ कर गुज़रने को फड़फड़ा रही है। हम दोनों ने दोस्ती भरी बातें की और।अलविदा के जाम टकराये। अगले दिन चोमा फिर आये। खड़े खड़े ही बोले ‘एक बार फिर आपको देखने का मन किया, चला आया। ‘ बेपनाह मोहब्बत थी दोनों में। हेंगेदुश काफी दूरी तक चोमा को छोड़ने के लिए गये। जब तक चोमा उनकी आंख से ओझल नहीं हो गए प्रोफेसर हेंगेदुश डबडबाई आँखों से उसे निहारते रहे।
यह तीर्थयात्री विद्वान अपनी एकाकी यात्रा पर 35 साल की उम्र में एक चुनौती भरी खोज में निकल पड़ा। उसने1सादे कपड़े पहने हुए थे तथा हाथ में एक छड़ी थी और बगल में एक छोटा सा झोला। नवंबर 1819 को इस एकांतवासी वीर ने हंगरी की पहाड़ी सीमा पार की। उद्देश्य था कांस्टेण्टिनोपल से एशिया में प्रवेश करना। लेकिन तुर्की में प्लेग का प्रकोप होने की वजह से अपना रास्ता बदलना पड़ा। अब वह यूरोपीय तट से होकर मिस्र पहुंचा। सिकंदरिया उतर कर कुछ समय तक अरबी भाषा का अध्ययन किया। वहां भी प्लेग की बीमारी आ पहुंची जिस के चलते चोमा सीरिया के अलेप्पो पहुंच गया। जहां भी चोमा जाते दो काम करते। एक तो वहां की स्थानीय भाषा सीखते और दूसरे वहां की पोशाक पहनते। इसके बाद परियों के देश बगदाद पहुंचे। कुछ पैदल चले तो कुछ यात्रा नाव से की। लेकिन बगदाद में परियों जैसा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया।अलबत्ता वहां के अंग्रेज़ रेजिडेंट से उन्हें आर्थिक सहायता मिली जिससे उनका आगे का सफर काफी हद तक आसान हो गया। उन दिनों एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए काफिले चला करते थे। ऐसे ही एक काफिले में शामिल होकर चोमा तेहरान पहुंच गया। वहां तक पहुंचने में करीब एक साल लग गया 14 अक्टूबर 1820 को एशिया की सरहद में पहुंच कर चोमा की आंखों में चमक आ गयी। उनकी योजना के अनुसार उन्हें आगे का रास्ता नहीं सूझा, पैसा भी खत्म हो चुका था। लिहाज़ा ब्रितानी दूतावास का दरवाजा खटखटाया जहां उन्हें सर हेनरी और मेजर जॉन विललोक मिले जो किसी एनजीओ से संबद्ध थे। उन्होंने चोमा की पैसों, कपड़ों और किताबों से मदद की। उनके संरक्षण में चार माह रहे। चोमा ने वहां दो प्रमुख कार्य किये। एक अपनी अंग्रेज़ी को मांझा और दूसरे फारसी बोलने की आदत डाली। मार्च 1821 को वहां से निकल कर चोमा ने अपना नाम बदल कर सिकंदर बेग रख लिया। भारत में अलेक्जांडर को सिकंदर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय कपड़े पहने और मुंह मंगोलिया की ओर किया। चोमा ने अपनी बची खुची पूंजी, अपने प्रमाणपत्र, अपना पासपोर्ट, अपने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा अपना यूरोपीय सूट अपने मददगारों के पास इस पुर्ज़े के साथ छोड़ दिया कि अगर मैं बुखारा के रास्ते मर जाऊं या फनाह हो जाऊं तो मेरी यह अमानत मेरे परिवार के पास पहुंचवा दीजिएगा। चोमा बुखारा तो पहुंच गया लेकिन यहां पहुंच कर अफवाह सुनी कि रूसी सेना की नाकेबंदी के कारण वह पूर्व की तरफ नहीं जा सकते।
बुखारा पहुंच कर भी अपनी मंज़िल की तरफ न बढ़ पाने का अफसोस चोमा को था लेकिन हालात के हाथों मजबूर था। तेहरान से फिर वह एक काफ़िले में शामिल हो गया जो काबुल जा रहा था। रास्ते में चोमा ने बल्ख, कुलम और बामियान भी देखा। बामियान में बुद्ध की वह मूर्ति भी देखी जो एक पहाड़ के किनारे चित मुद्रा में थी। बुद्ध की इस मूर्ति ने उन्हें ऐसा आकर्षित किया कि चोमा टकटकी लगाए काफी देर तक उसे देखते रहे। चोमा विलक्षण प्रतिभा के तो थे ही उन्होंने मध्य और पूर्वी एशिया की संपन्न और समृद्ध संस्कृति का अनुभव किया होगा। दूसरे वह इतिहास के छात्र रहे हैं इसलिए बुद्ध की मूर्ति से जुड़े प्रसंग भी आसानी से समझ में आ गए होंगे। वैसे उस समय एशिया था भी ज्ञान का भंडार, यूरोपीय सैलानी औऱ छात्र यहां आना अपना अहोभाग्य समझा करते थे। लेकिन चोमा को काबुल अपने अनुकूल नहीं लगा लिहाज़ा वह पेशावर जाने वाले काफिले में शामिल हो गया।
रास्ते में चोमा दो फ्रेंच जनरलों अल्लार्ड और वेंतूर से मिले जो महाराजा रणजीत सिंह की सेना में थे। भाषाविद चोमा को इन फ्रेंच जनरलों ने अपने साथ लाहौर चल कर महाराजा रणजीत सिंह से मिलने का मशविरा दिया। चोमा बारह दिनों तक इन जनरल द्वय के साथ लाहौर में रहे। उनके महाराजा रणजीत सिंह से मुलाकात करने या न करने पर जब मैंने अपनी दुविधा का इज़हार अपने लाहौर के दौरे में पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष अस्मा जहांगीर से किया तो उन्होंने बताया कि चोमा की महाराजा से न केवल मुलाकात हुई थी बल्कि उनकी प्रतिभा से वह इतने चमत्कृत हुए थे कि उन्हें अपने दरबार में रहने का प्रस्ताव तक दिया था। लेकिन चोमा के दिलोदिमाग पर तो पुरखों की मूलभूमि तलाशने की धुन सवार थी , उन्होंने ने बड़ी विनम्रता से सधन्यवाद इस प्रस्ताव को स्वीकारने में अपनी असमर्थता जता दी। अलबत्ता लाहौर में उनकी आंखें ज़रूर कुछ तलाशती नज़र आयीं।
लाहौर से चोमा ने लद्दाख की राह ली। उनका मकसद लद्दाख की राजधानी लेह से होकर यारकंद पहुंचना था। लेह जाकर चोमा को पता चला कि यारकंद पहुंचना न केवल कठिन और असाध्य है बल्कि बहुत महंगा भी। अहम और आत्म सम्मान चोमा में कूट कूट कर भरा हुआ था। किसी के आगे उन्हें हाथ पसारना गवारा नहीं था। इसी उधेड़बुन में चोमा लद्दाख में घूमता रहा।सौभाग्य से चोमा की मुलाकात एक अंग्रेज़ सैलानी जॉर्ज मूरक्राफ्ट से हो गयी जो उनकी तरह ही जिज्ञासु प्रकृति के थे। दोनों में पटरी इसलिए भी बैठी कि दोनों यूरोपीय थे और भाषाविद भी। मूरक्राफ्ट को चोमा ने अपना मकसद बताया। मूरक्राफ्ट ने उन्हें सलाह थी कि पहले वह तिब्बती भाषा का अध्ययन करें।उन्होंने चोमा को 1762 में प्रकाशित फादर गिएओरगी की तिब्बती वर्णमाला की एक किताब सौंपते हुए कहा कि इससे तुम्हें कुछ मदद मिल जाएगी। चोमा की मदद के लिए मूरक्राफ्ट ने कुछ परिचय पत्र और पैसे भी दिये ताकि वक़्त ज़रूरत पर वे उनके काम आ सकें। उन्होंने चोमा को बताया कि उनका फ़ारसी का ज्ञान तिब्बती सीखने में सहायक होगा। तिब्बती सीखने के लिए उन्होंने अपने एक तिब्बती लामा मित्र सांग्स-रग्यास फुन-तशोग्स के नाम पत्र देते हुए कहा कि वह अनेक विधाओं का विशेषज्ञ है तिब्बती औऱ फ़ारसी सहित। मूरक्राफ्ट कई बरसों से लद्दाख में काम कर रहा था इसलिए उसकी जान पहचान का दायरा खासा व्यापक था। चोमा और मूरक्राफ्ट के बीच एक समझौता हुआ जिसके अनुसार चोमा तिब्बती भाषा में शब्दकोश और व्याकरण तैयार करेंगे। इस समझौते की एक प्रति भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में भी सुरक्षित है। इस समझौते को लेकर भी कई तरह की शंकाएं व्यक्त की गयीं। कुछ लोग मूरक्राफ्ट को ब्रिटिश गुप्तचर करार देते हुए कहा करते थे वह चोमा का गुप्तचरी में इस्तेमाल कर रहे हैं और चोमा को उसके मूल मिशन से भटकाना चाहता है। किसी भी दौर में इस तरह की भ्रांतियां फैलाया जाना आम बात होती है। मैंने अपने कुछ जानकारों से मूरक्राफ्ट के काम के बारे में पता किया तो मुझे बताया गया कि मूरक्राफ्ट एक पशु चिकित्सक था और उसका काम कंपनी के लिए अच्छी नस्ल के अरबी घोड़े खरीदनाहुआ करता था। इंग्लैंड में इस नस्ल के घोड़े बमुश्किल मिलते हैं और बहुत महंगे होते हैं। मूरक्राफ्ट आसपास के देशों में घूमता रहता था और उसकी पहुंच काफी ऊपर तकहुआ करती थी । उसका लद्दाखी राजा औऱ महत्वपूर्ण लामाओं पर भी खासा प्रभाव था। हंगरी में ही कुछ लोगों ने बताया कि चोमा और मूरक्राफ्ट एक ही किश्ती के दो सवार हैं जो लद्दाख में आकर मिल गये।दोनों ही खोजी प्रकृति के असाधारण व्यक्ति थे।मूरक्राफ्ट चोमा के हंगरी से पैदल चलकर कश्मीर पहुंचने को किसी’चमत्कार’ से कम नहीं मानते थे। अलावा इसके चोमा और उनके बीच हुए समझौते के तहत शब्दकोश और व्याकरण का काम भारत सरकार के लिए किया जा रहा था। जो पैसे और परिचय पत्र उन्होंने चोमा को दिए थे वह उनके अदभुत और महत्वपूर्ण कार्य में मदद करने के लिये। वह भी यह जान गए थे कि चोमा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मूरक्राफ्ट ने तो चोमा के बारे में कहा है कि अपने देश की मूलभूमि की खोज में कोई इंसान जो इतना प्रतिभशाली ,साहसी, दूरदर्शी और अपने जुनून के प्रति समर्पित हो’पागलपन’ की इस हद तक जा सकता है इसकी मिसालें परिकथाओं में तो पढ़ी गयी होंगी, हक़ीक़त में उसे देखना और जानना किसी अजूबे से कम नहीं। मूरक्राफ्ट ने तो यहां तक व्यवस्था कर दी थी कि काम खत्म होते ही चोमा पांडुलिपि लेह में छोड़ कर अपनी यात्रा आगे शुरू कर सकते हैं।
मूरक्राफ्ट की व्यवस्था के अनुसार चोमा तिब्बती भाषा के अध्ययन के लिए जांगला के लामा से जांस्कर में मिला। दोनों ने 23 जून, 1823 से 22 अक्टूबर, 1824 तक तिब्बती भाषा और साहित्य का अध्ययन किया। वहां की कई मोनास्ट्रीइज़ यानी मठों में उपलब्ध और कहीं कहीं बिखरे पड़े साहित्यिक भंडार को देखकर चोमा की आंखें चौंधिया गयीं। यह साहित्यिक खज़ाना 320 बड़े आकार की किताबों के रूप में छपा हुआ था। पहले छह माह चोमा ने अपने लामा साथी के साथ एक ऐसे स्थान में गुज़ारे जिसे आप ठंडा मरुस्थल कह सकते हैं। रात को कड़ाके की ठंड में उकड़ू होकर सोते। कहीं से भी रोशनी मिलती पढ़ना शुरू कर देते। जांगला का लामा सांग्स-रग्यास फुन-तशोनग बहुत ही विद्वान था। उन्हें बहुश्रुत इस मायने में कहा जाता था कि वह तिब्बत औऱ नेपाल के धर्म की सभी विधाओं से परिचित थे। चिकित्सा, खगोल शास्त्र और ज्योतिष उनका प्रोफेशन था, अर्थव्यवस्था में वह पारंगत बताये जाते थे, सामान्य ज्ञान में उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, दूर दराज के लोग उनसे इलाज कराने आते थे औऱ वह दलाई लामा के भी निजी चिकित्सक थे। ऐसे विद्वान लामा के साथ चोमा को 1823 से 1830 तक का साथ मिला। उनके साथ चोमा ने जांगला, फुकटल और कानाम मठों में रहकर तिब्बती साहित्य का गहन अध्ययन किया। सर्दी से बचने के लिए ये लोग सतलुज की घाटी भी चले जाते या सबाथू में जो ब्रितानी पहाड़ी छावनी थी। यहीं वह अपने साथ 320 किताबों का सारांश भी ले जाते। सबाथू में राजनीतिक ऑफिसर कैप्टेन कैनेडी का उन्हें पूरा समर्थन मिलता। कैप्टेन कैनेडी को ही शिमला का संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार 30 हज़ार शब्दों की तिब्बती-अंग्रेज़ी शब्दकोश तैयार हो गया, तिब्बती व्याकरण भी पूर्ण हो गयी तथा तिब्बती साहित्य और इतिहास की एक अन्य पुस्तक भी। मूरक्राफ्ट तो इस बीच चल बसे लेकिन चोमा के लिए हर जगह रास्ता बना कर गये।
चोमा के चेहरे पर एक चमक थी जो उनके महत्वपूर्ण, परिश्रमी, प्रतिबद्धता भरे ऐतिहासिक कार्य की थी, पैसे की नहीं। सम्मान तो उनकी मेहनत और लगन को कई तरह1से प्राप्त हो चुके थे लेकिन चोमा के अथक परिश्रम का श्रेय एशियाटिक सोसाइटी और सरकार ने कुछ ज़्यादा ही ले लिया। संत विद्वान कहे जाने वाला चोमा हिब्रू, अरबी, संस्कृत, पश्तो, ग्रीक, रूसी, लैटिन, स्लावोनिक, जर्मन, इंग्लिश, तुर्की, फ़ारसी, फ्रेंच, तिब्बती , हिंदुस्तानी, बंगला, मराठी, मैथिली भाषाओं का जानकार था। चोमा ने अपने जीवन के पहले 35 साल यूरोप में अपनी यात्रा की तैयारी में लगाये, 12 बरस पैदल यात्रा करने और बौद्ध लामा के साथ अध्ययन में तथा आखिरी के 11वर्ष भारत में सामग्री एकत्र करने, लिखने ,छपवाने और सरकार को सौंपने में। 1842 में चोमा को पुनः यात्रा की सनक सवार हुई लेकिन इससे पहले वह अमली जामा पहन पाती 11 अप्रैल, 1842 को दार्जीलिंग में उनका निधन हो गया।
(17-18 जून 2020 को लिखी त्रिलोक जी की ये पोस्ट फेसबुक से साभार)
Posted Date:June 29, 2020
3:55 pm Tags: त्रिलोक दीप, लद्दाख, चोमा





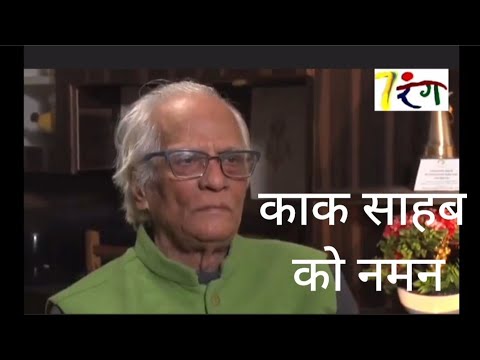











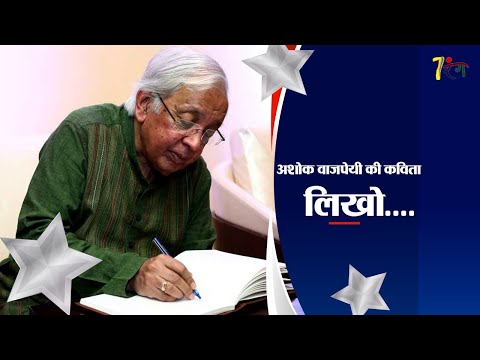








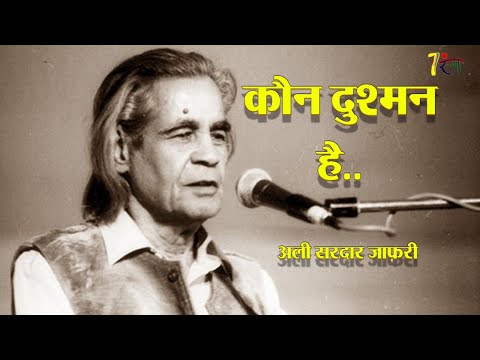
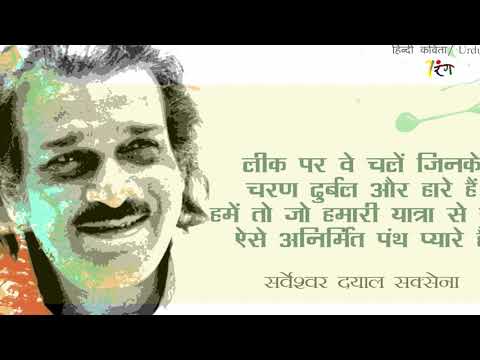



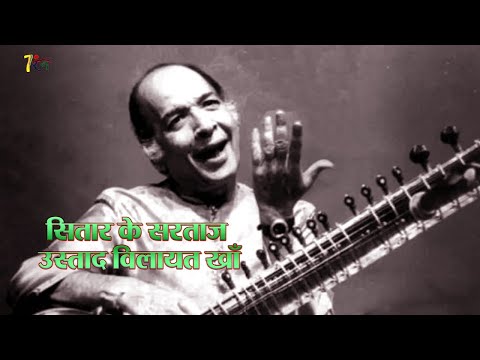






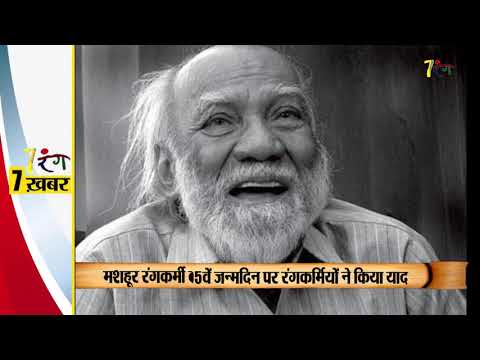















One thought on “जब त्रिलोक दीप पहली बार लद्दाख़ गए…”
Comments are closed.