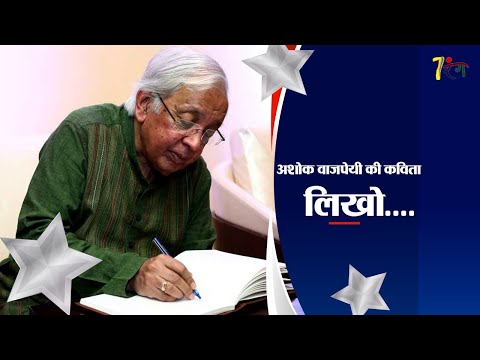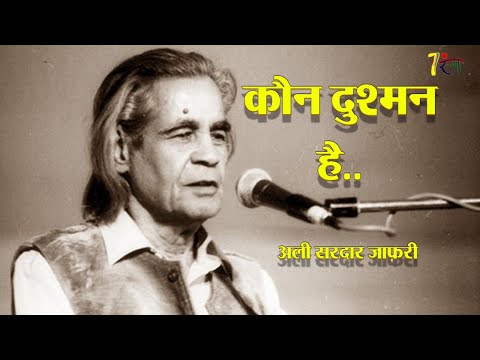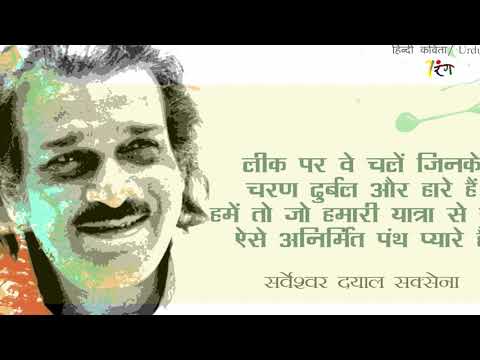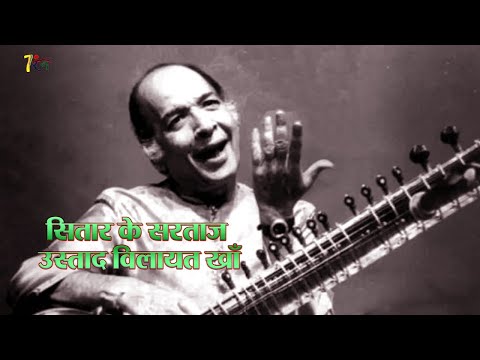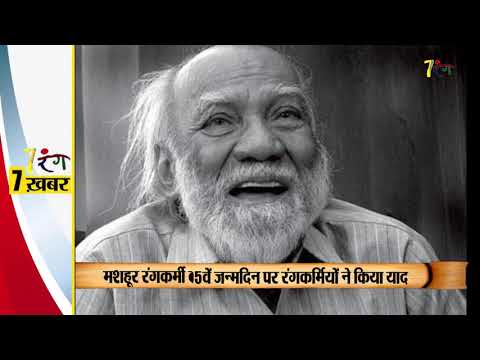वाराणसी के जाने माने रंगकर्मी गोपाल गुर्जर की बेशक कोई राष्ट्रीय पहचान न बन पाई हो लेकिन उनकी प्रतिभा को रंग जगत और सिने जगत ने कुछ हद तक पहचाना जरूर। उनका गुज़रना कम से कम वाराणसी रंगमंच की दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है। संवेदनशील पत्रकार और ‘नाद रंग’ पत्रिका के संपादक आलोक पराड़कर ने गोपाल गुर्जर को ‘राष्ट्रीय सहारा’ में लिखे अपने लेख के ज़रिये कुछ इस तरह याद किया.. 7 रंग के पाठकों के लिए हम वह लेख साभार पेश कर रहे हैं।
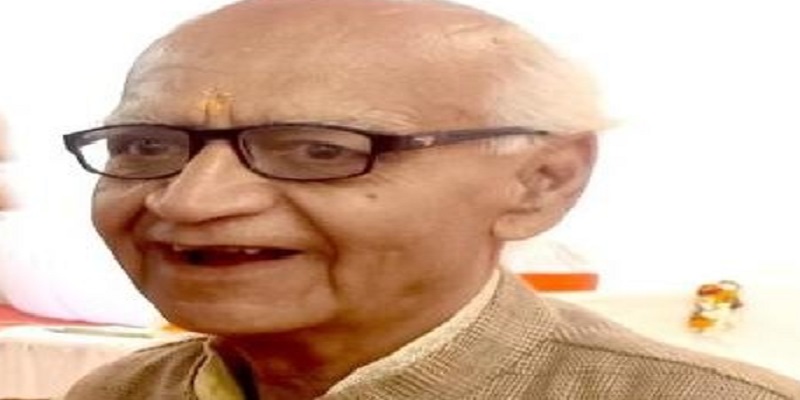
इन दिनों कोरोना संकट ही खबर है। ऐसे में गोपाल गुर्जर जैसे रंगकर्मी के न रहने की सूचना स्थानीय स्तर से बाहर आती भी तो कैसे लेकिन ये तो सोशल मीडिया है जो साझा मित्रों के जरिए ऐसी बातों का पता चल जाता है। वैसे भी गोपाल गुर्जर की पहचान ऐसी नहीं थी कि उनके निधन की चर्चा आम दिनों में भी राष्ट्रीय स्तर पर हो पाती। पूरा जीवन नाटकों में लगा देने के बावजूद उनका कद इतना बड़ा नहीं समझा गया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने कुछ वर्षों पूर्व उन्हें अकादमी सम्मान जरूर दिया था लेकिन लखनऊ के रंगकर्मी या रंगप्रेमी भी उन्हें ठीक से शायद ही जानते हों। दूसरे शहरों में भी उन्हें जानने वाले काफी कम ही होंगे।
लेकिन बनारस में उनकी धाक जरूर थी। वहां का रंग परिदृश्य पिछले कई दशकों से उनके बिना मुकम्मल नहीं होता था। वे लगातार नाट्य प्रस्तुतियां करते थे। मंच प्रस्तुतियों से इतर आकाशवाणी के नाटकों में भी वे एक जरूरी कलाकार थे। कहा तो ये भी जाता है कि आकाशवाणी के लिए नाटक लिखते समय कई नाटककार ये सोचकर नाटक लिखा करते थे कि इसमें गोपाल गुर्जर की भूमिका क्या होगी। राम पदारथ राय के साथ उनकी जोड़ी भी खूब लोकप्रिय थी। उन्होंने दो सौ से अधिक रेडियो नाटकों में काम किया था। कुछ वर्षों पूर्व राय के निधन से यह जोड़ी टूट गई थी। मंच पर उन्होंने ज्यादातर नाटक नागरी नाटक मंडली के साथ किए।
रंगमंच में उनकी यह उपस्थिति उन्हें बनारस में होने वाले धारावाहिकों और फिल्मों से भी जोड़ देती थी। बनारस में शूटिंग का सिलसिला अक्सर चलता रहता है। हालांकि ये छोटी-छोटी भूमिकाएं ही थीं। फिल्मों या धारावाहिकों में कोई ऐसी भूमिका उन्हें नहीं मिली जिसने उनके अभिनय को बनारस से बाहर व्यापक पहचान दी हो। लेकिन उन्हें जानने वाले उन्हें इनमें देखकर खुश जरूर हो लेते थे। घातक, तुलसीदास, लागा चुनरी में दाग, मोहल्ला अस्सी, मसान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान ऐसी फिल्में थीं।
गोपाल गुर्जर का वास्तविक नाम एम.एन.गुर्जर (मानेश्वर नाथ गुर्जर) था। इस 22 मार्च को जब उनका निधन हुआ वे 87 साल के थे। उन्होंने भरा-पूरा जीवन जिया और आखिरी समय तक उनकी सक्रियता बनी रही। उनके घासीराम कोतवाल, मकान नंबर 144, सुनयना, तस्वीर, द ग्रेट राजा मास्टर जैसे नाटकों की काफी चर्चा होती है। उनके साथ कई नाटकों में कई काम कर चुके दूरदर्शन अधिकारी रहे, बनारस के ही नरेन्द्र आचार्य कहते हैं, ‘वे बहुत स्वाभाविक अभिनय तो करते ही थे, लंबे-लंबे संवाद याद करने में उन्हें महारत थी। एक बांग्ला फिल्म के लिए अभी कुछ समय पहले तीन पन्ने का संवाद उन्होंने एक टेक में ही ओके कराकर उन्होंने हम सबको चौंका दिया था। उनका समर्पण हम सबको प्रेरित करता था।’
गोपाल गुर्जर सन् 1974 में बनारस आए थे। इसके पहले वे गया और फिर थोड़े समय के लिए दिल्ली भी रहे। दिल्ली में उन्होंने गीत एवं नाटक प्रभाग में काम किया। बनारस आकर उन्होंने रामघाट स्थित सांगवेद विद्यालय में नौकरी कर ली थी और फिर इसी से जुड़े रहे।
गोपाल गुर्जर के नाटकों को देखते हुए मैंने महसूस किया था कि उन पर ऐसी भूमिकाएं खूब फबती थीं जिनमें एक मध्यमवर्गीय परिवार की चिड़चिड़ाहट या खीझ को अभिव्यक्त करना हो। उन्हें याद करते हुए उनका वही चेहरा, वही अभिनय आंखों के सामने आ जाता है। रेडियो नाटकों में भी अक्सर उनके संवाद बोलने का अंदाज ऐसा ही होता था। ये चिड़चिड़ाहट या खीझ क्या थी, क्या यह उनके भीतर का गुस्सा था जो अभिनय में अक्सर उभर कर आ जाता था और क्या यह चिड़चिड़ाहट या खीझ हर उस रंगकर्मी की नहीं है जो छोटे-छोटे शहरों में रंगकर्म करते हैं, सराहे जाते हैं लेकिन कभी राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई गिनती नहीं हो पाती है।
उनकी कला उनके अपने शहर के दायरे से बाहर जाकर स्वीकृति नहीं पा पाती है। बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, शाहजहांपुर, आजमगढ़ जैसे शहरों में गोपाल गुर्जर जैसे कितने ही रंगकर्मी हैं जिन्होंने अपना जीवन रंगमंच को समर्पित कर दिया है। ये वे लोग हैं जिनमें युवावस्था में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दिल्ली चले जाएं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश की कोशिशें कर सकें। उनके लिए तब उनके घर-परिवार की जिम्मेदारियां अधिक महत्त्वपूर्ण थीं लेकिन उन्होंने रंगमंच के अपने शौक को बनाए रखा। पढ़ाई की और फिर छोटी-बड़ी अपनी नौकरियां या व्यवसाय किया लेकिन अपनी आग को बचाए रखा। भाग-भागकर रिहर्सल में आते रहे, कभी अपने परिवारीजनों से छुपकर तो कभी अपने अधिकारियों से बचकर। आर्थिक सुरक्षा जरूरी थी, अपने और परिवार के लिए भी लेकिन अगर अच्छी नौकरियां मिल गई तो पहले रिहर्सल और प्रदर्शनों के लिए जैसे-तैसे बहाने किए और फिर जल्द से जल्द स्वैच्छिक अवकाश लेकर रंगमंच में पूरी तरह रम गए। नाटकों के प्रदर्शन के लिए कई बार घर से पैसा लगाया, महिला कलाकारों की कमी हुई तो अपनी बहन-बीवी को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।
हिन्दी रंगमंच की स्थिति आज भी ऐसी नहीं है कि इन शहरों में केवल रंगमंच करते हुए जीवन यापन का प्रबंध किया जा सके। अनुदान का पैसा भी इन शहरों में आता है लेकिन उसका अपना गणित है। कुछ वर्षों पूर्व लखनऊ में मेरी भेंट सुगंधा से हुई थी जिसका चयन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए हुआ था। सुगंधा ने बताया था कि उसने अपने परिवार से छुपकर रंगमंच किया है और परिवारवालों को इस चयन के बारे में भी नहीं मालूम था। वह चाहती थी कि परिवारवालों को यह बताया जाए कि रंगमंच भी एक सम्मानजनक कार्य है जिससे वे उसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का प्रशिक्षण लेने से रोके नहीं। मुझे नहीं पता कि बाद में सुगंधा अपने परिवार को कैसे राजी कर सकी लेकिन इस प्रसंग से यह जरूर स्पष्ट हुआ कि हिन्दी रंगमंच को लेकर समाज में स्थिति आश्वस्तिपरक नहीं है। कोई भी परिवार अपने बेटे-बेटी का भविष्य उसमें नहीं देख पाता। ऐसे में रंगमंच के शौक को जीवन भर बचाए रख पाना निश्चय ही काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है लेकिन इससे जो सन्तुष्टि और खुशी मिलती है, वह ऐसे रंगकर्मियों को इस कला से जोड़े रखती है। सच्चाई यही है कि इन शहरों में हिन्दी रंगमंच, जो शौकिया रंगमंच है, ऐसे ही रंगकर्मियों के कारण जीवित है। हिन्दी रंगमंच के इतिहास में हो सकता है कि ऐसे रंगकर्मियों को रेखांकित न किया जाए लेकिन उनके बिना वह पूरा भी नहीं होता!
(राष्ट्रीय सहारा से साभार)
Posted Date:April 7, 2020
12:52 pm Tags: Alok Paradkar, आलोक पराड़कर, गोपाल गुर्जर, रंगकर्मी गोपाल गुर्जर, वाराणसी रंगकर्म, Gopal Gurjar, Varanasi Gopal Gurjar