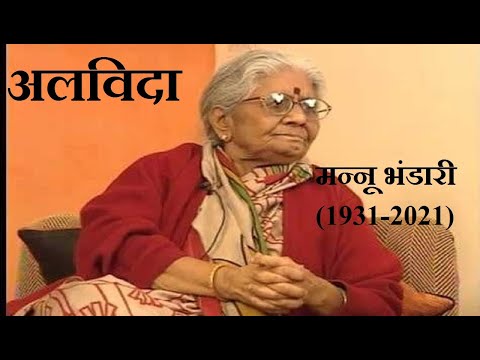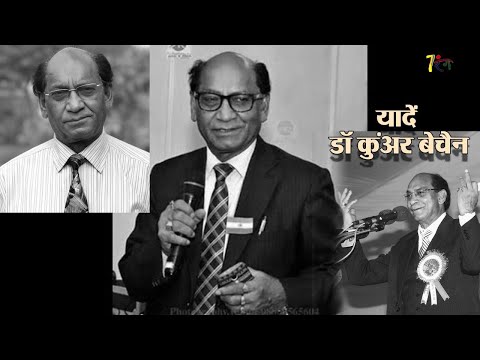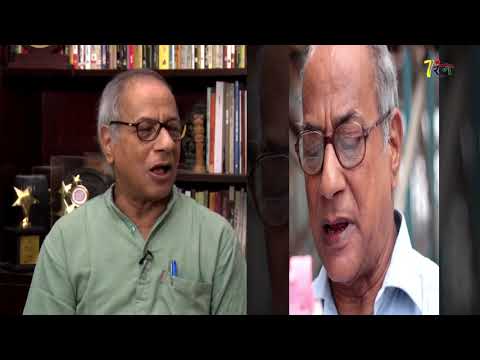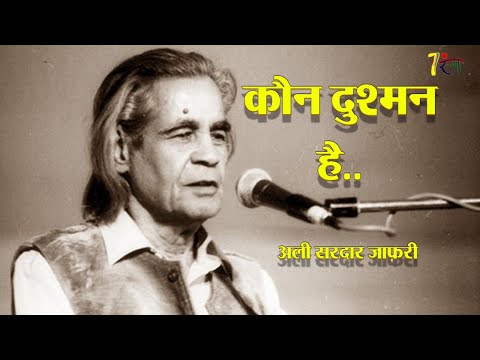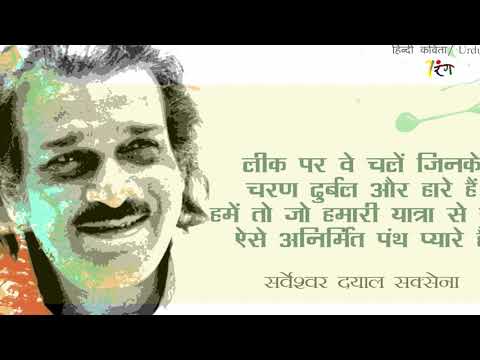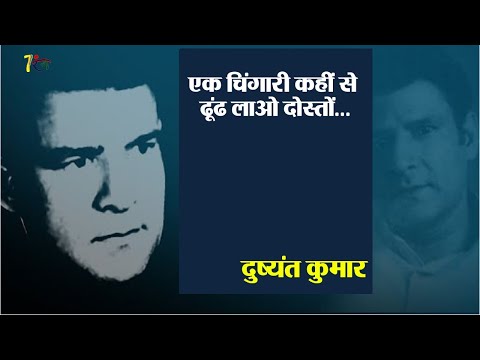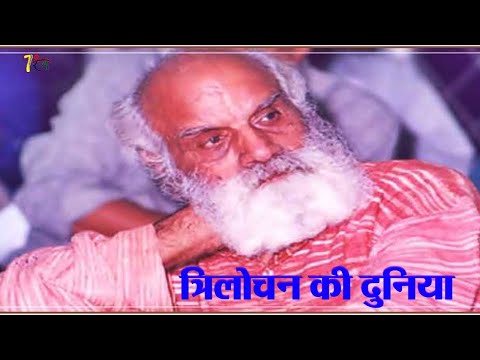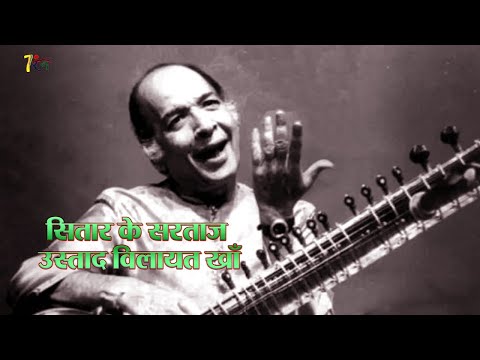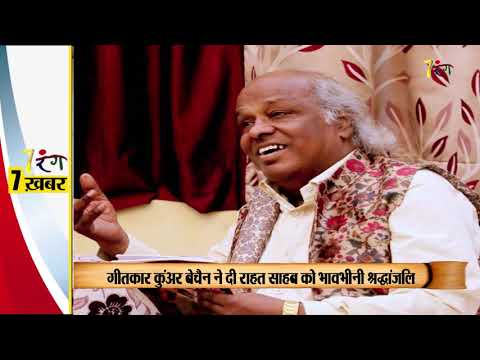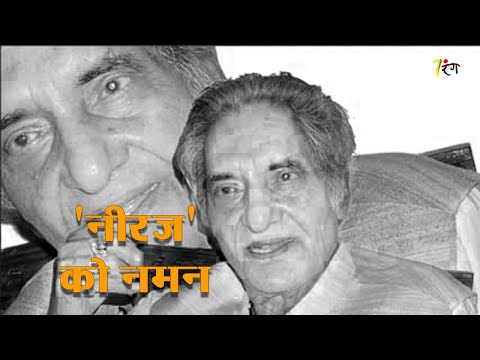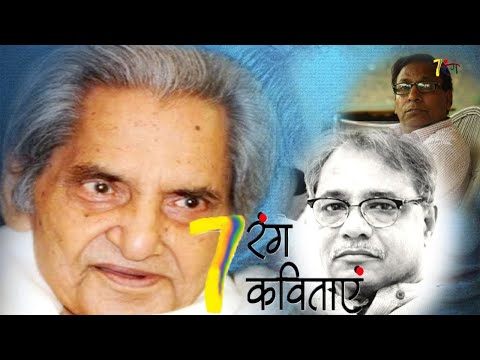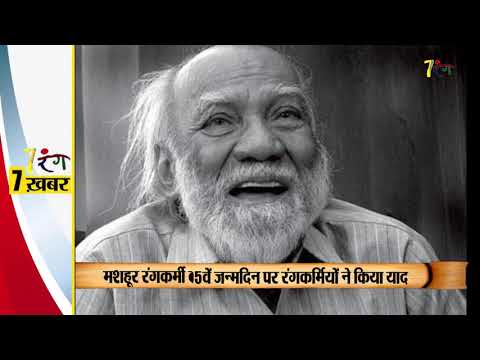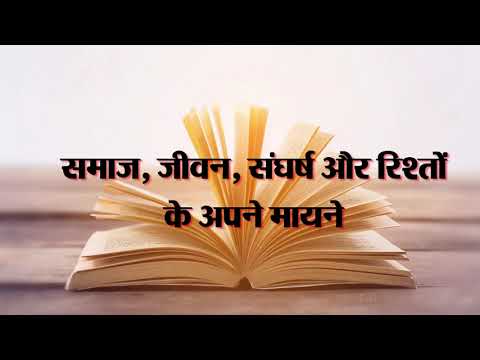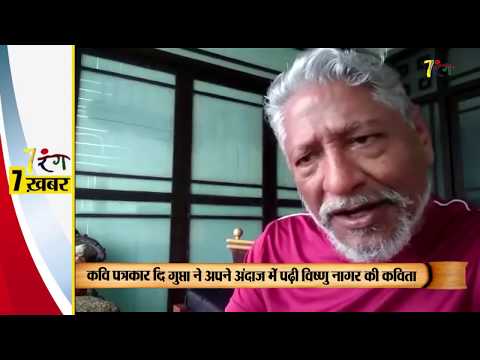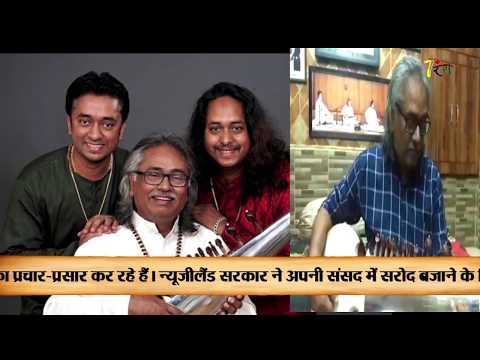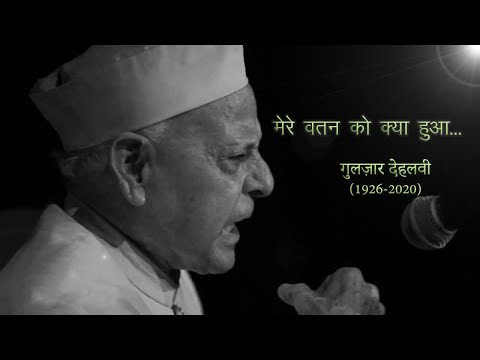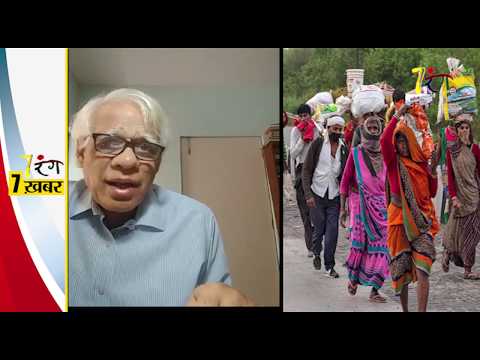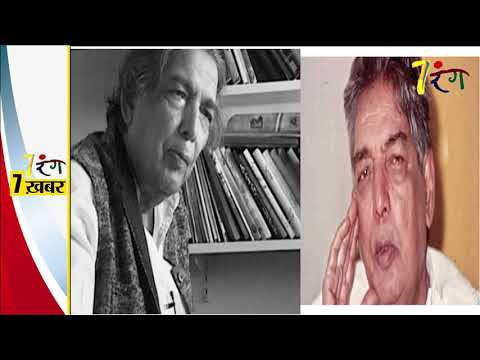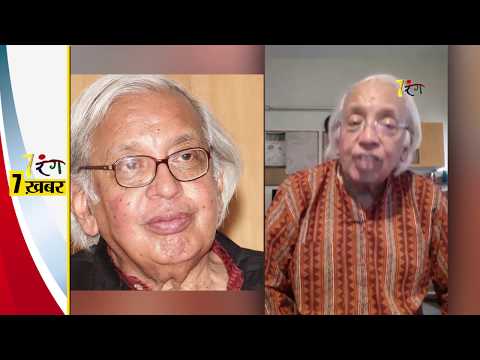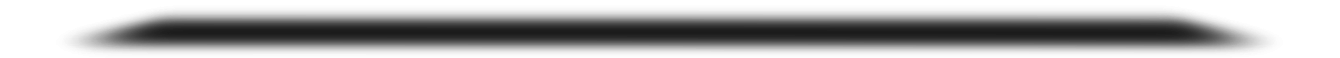“स्त्री विमर्श “का “जोगिया राग”
हिंदी रंगमंच में आजकल बहुत कम ऐसे नाटक देखने को मिलते हैं जिनकी प्रस्तुति पूरी तरह से हर पैमाने पर खरी उतरे और उसमें एक कसाव हो। किसी नाटक का सफल होना केवल निर्देशक पर निर्भर नहीं करता बल्कि अभिनेता और नाटक के चुस्त संवादो पर भी निर्भर करता है। कहानी के रंगमंच के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर “ मेलो रंग” की ओर से प्रस्तुत विजय पंडित का “जोगिया राग “ एक ऐसा ही नाटक है जो अपनी प्रस्तुति में पूरी तरह से “कॉम्पैक्ट” नाटक है। उसमें किसी तरह का कोई असंतुलन नहीं है और उसका हर दृश्य बंध अर्थपूर्ण है, सफल है।
दरअसल विजय पंडित का यह नाटक एक ग्रामीण स्त्री के जीवन में गृहस्थ कामना की पुकार की कहानी है। कैसे सावित्री नामक एक ग्रामीण स्त्री अपना वैवाहिक जीवन जीना चाहती है पर अपने ब्राह्मण पति के “जोगी” बन जाने के कारण वह एक अधूरा जीवन 15 साल तक गुजारती है, फिर नियति उसके साथ एक खेल करती है और जीवन के फूल खिलते हैं उसमें खुशबू आती है।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक एवं “कहानी का रंगमंच” के प्रणेता देवेंद्र राज अंकुर द्वारा निर्देशित यह नाटक बहुत दिनों तक नाटक प्रेमियों के मन मस्तिष्क पर छाया रहेगा। इस नाटक ने दर्शकों पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसकी स्मृति वर्षों तक महफूज रहेगी। इस नाटक ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर नाटक का कथ्य मजबूत हो और अभिनेता अपने अभिनय से उस कथ्य को उजागर कर दे तो यह नाटक दर्शकों के मन पर अपनी अमिट छाप जरूर छोड़ता है।
अंकुर ने इस नाटक की समाप्ति पर खुद स्वीकार किया इस नाटक के दोनों अभिनेता इतने सशक्त हैं कि वह इस नाटक को खुद अपने कंधों पर संभाले हुए है कि उन्हें एक निर्देशक के रूप में कुछ अधिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्वीकार किया कि यह नाटक 90% इन दोनों अभिनेताओं ने खुद संभाल रखा है और इसमें निर्देशक की मदद की आवश्यकता नहीं पड़ी, हालांकि यह अंकुर जी की विनम्रता है कि उन्होंने इस नाटक का सर्वाधिक श्रेय अभिनेताओं को दिया है। वैसे इस नाटक में केवल दो पात्र हैं और एक साड़ी है। बस एक साड़ी के सहारे इस नाटक को खड़ा किया गया। वह एक स्त्री के जीवन उसकी त्रासदी उसकी वेदना का एक प्रतीक बन जाता है। इस नाटक के दोनों अभिनेता निधि और मुक्ति राष्ट्रीय नाटक विद्यालय के छात्र चुके हैं और उन दोनों ने अपने अभिनय क्षमता से इस नाटक को बांधे रखा और कहीं से यह लचर या ढीला नहीं रहा। वह इतना चुस्त और दुरुस्त नाटक रहा कि नाटक का कथ्य अपने आप उभर कर सामने आया ।
अक्सर देखा गया है कि कई बार किसी नाटक का संगीत तत्व या सेट या संवाद इतना लाउड हो जाता है कि नाटक एक कलात्मक प्रस्तुति नहीं बन पाती है, लेकिन जोगिया राग नामक कहानी का नाट्य रूपांतरण इतना सधा हुआ है कि इसमें दर्शक बोर नहीं होता है।
कहानी का सार यह है कि सावित्री नामक एक ग्रामीण स्त्री की शादी एक ब्राह्मण परिवार के बालमुकुंद तिवारी नामक एक युवक से होती है लेकिन उस युवक के प्रारब्ध में “योगी” बनना लिखा होता है और वह अपना वैवाहिक जीवन त्याग कर एक दिन घर से बाहर निकल जाता है।इस तरह वह 15 वर्षों तक लौटकर नहीं आता है जबकि सावित्री उसके लौटने का इंतजार करती है और अपने सुहाग की रक्षा करती है। उसे विश्वास है कि एक दिन उसका पति जरूर लौटेगा और तब वह अपने शेष बचे वैवाहिक जीवन को सफलता से गुजरेगी। इस बीच गांव और बिरादरी के लोग उससे कहते हैं कि अब उसके परिवार वालों को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि उसका पति अब नहीं रहा और सावित्री को अब एक विधवा जीवन जीना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण परिवार में स्त्री के लिए दूसरा जीवन स्वीकार्य नहीं है लेकिन सावित्री ऐसा नहीं करने देती है। वह मानती भी नहीं है कि उसका पति अब नहीं रहा। 15 वर्ष के बाद उसे पता चलता है एक पड़ोसी गांव में योगियों का एक दल आया है और वह इस उम्मीद में उस गांव में जाती है ताकि उसे उस दल में कहीं अपने पति से वहां मुलाकात हो जाए। जब पंचायत के पास बात पहुंचती है तो सावित्री को जोगियो के दल से मिलवाया जाता है और वहां सावित्री एक दूसरे योगी को अपना पति बालमुकुंद समझकर पूछती है – क्या तुम अब गृहस्थ जीवन में नहीं लौटोगे, अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभालोगे। वह व्यक्ति सावित्री की बातों को मान लेता है और सावित्री के साथ वैवाहिक जीवन स्वीकार लेता है लेकिन जब वह व्यक्ति घर पर आकर सावित्री से कहता है कि वह बालमुकुंद नहीं है बल्कि एक खुद योगी है तो फिर सावित्री को बड़ी निराशा होती है लेकिन वह योगी यह भी कहता है कि वह खुद ही बचपन में 10 -11 वर्ष की अवस्था में “जोगी” बनकर घर से बाहर निकल गया था और गांव-गांव घर-घर भटकने के बाद इतना ऊब गया कि उसके अंदर एक गृहस्थ जीवन की कामना जागी और इसीलिए जब सावित्री ने उसे अपना पति बालमुकुंद समझ कर वैवाहिक जीवन की ओर लौटेने बात कही तो उसने यह स्वीकार लिया। हालांकि थोड़ी देर के लिए सावित्री को झटका जरूर लगता है लेकिन वह इस दोबारा जीवन को स्वीकार कर लेती है और उस व्यक्ति के साथ अपना शेष जीवन बिताने के लिए राजी हो जाती है। एक सुखांत नाटक है लेकिन इस नाटक में एक स्त्री के कई जीवन प्रसंगों, द्वंदों, विडम्बनाओं और सामंती मूल्यों में छिपी उसकी मार्मिक कथा को पेश किया जाता है। यह नाटक दरअसल स्त्री विमर्श का एक जोगिया राग है जो आज भी गांव में एक स्त्री की दुखद कहांनी कहता है।
देवेन्द्र राज अंकुर ने 1975 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल की ओर से संगीत नाटक अकादमी के स्टूडियो थिएटर में निर्मल वर्मा की तीन कहानियां को मिलाकर तीन एकांत से “कहानी का रंगमंच “ शुरु किया था और देखते-देखते इन 50 वर्षों में उन्होंने सैकड़ो कहानियों को रंगमंच पर प्रस्तुत कर एक नई विधा को जन्म दिया। इससे अंकुर को ख्याति ही नहीं मिली बल्कि हिंदी रंगमचं भी काफी समृद्ध हुआ और हिंदी कहानी के विविध रंगों को भी रंगमंच पर देखने का अवसर प्रदान हुआ।
अंकुर जी ने अपना यह रंगमंच “ साधन हीन रंगमंच” के रूप में विकसित किया .दरअसल पोलैंड के विश्व प्रसिद्ध रंगकर्मी ग्रोटेवस्की ने पश्चिम में “poor theatre” की अवधारणा विकसित की जिसके आधार पर ऐसे कई नाटक खेले गए जिसमें रंगमचं के न्यूनतम साधनों का इस्तेमाल किया गया। यह एक ऐसी अवधारणा थी जिसके जरिए कोई नाटक सीमित साधन में भी खेला जा सकता था। इसमे सेट डिज़ाइन, म्यूजिक और कॉस्ट्यूम की भी अधिक जरूरत नहीं थी।
प्रसिद्ध कवि एवं संस्कृतिकर्मी अशोक वाजपेयी ने नाटक के प्रारंभ में अपने उद्बोधन में कहा कि एक बार उनकी मुलाकात प्राग से बुडापेस्ट जाते हुए विमान में ग्रोटौव्स्की से हुई थी और उन्होंने अपने “poor theatre “ की अवधारणा पर बात करते हुए कहा था कि उन्होंने भारत के संस्कृत रंगमंच से इसकी प्रेरणा पाई और उन्होंने पश्चिम में इस अवधारणा को विकसित किया।
उन्होंने कहा कि इस रंगमंच को हम “साधनहीन रंगमंच” कह सकते हैं जहां कोई ताम झाम न हो और हम न्यूनतम साधनों से मंचन करते हैं।
उन्होंने कहा कि रंगमंच एक तरह का टीमवर्क है जिसमें नाटककार, अभिनेता, निर्देशक और ग्रीन रूम में काम करने वाले दल के लोग भी शामिल हैं।
उन्होंने भी कहा कि रंगमंच संवाद की विधा है। इसमें हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते बल्कि तादात्म्य स्थापित करते है। इसमें हम और मैँ का द्वैत है। नाटक दरअसल प्रश्न वाचक विधा है। उसमें हम प्रश्न करते हैं। आज के समय में जब राज्य का आतंक बढ़ गया हो प्रश्नों को पूछने में लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है वैसे में रंगमंच अपनी बात अपनी विधा के जरिए कह दे रहा है। वह नैतिक, मानवीय और सभ्य होने का पाठ पढ़ा रहा है।
उन्होंने इस बात पर अचरज व्यक्त किया की देवेन्द्र राज अंकुर ने किस तरह “कहानी के रंगमंच” के 50 वर्ष गुजर दिए जबकि आधुनिक रंगमंच का इतिहास 100 साल का रहा है। रज़ा फाउंडेशन और अन्य संस्थाओं की मदद से “ कथा रंग” का यह सप्ताह आयोजित किया जा रहा है।
वरिष्ठ पत्रकार, कवि औऱ रंग समीक्षक विमल कुमार की रिपोर्ट
Posted Date: April 27, 2025
10:05 am Tags: अशोक वाजपेयी, देवेन्द्र राज अंकुर, जोगिया राग, नाटक जोगिया राग, कहानी का रंगमंच