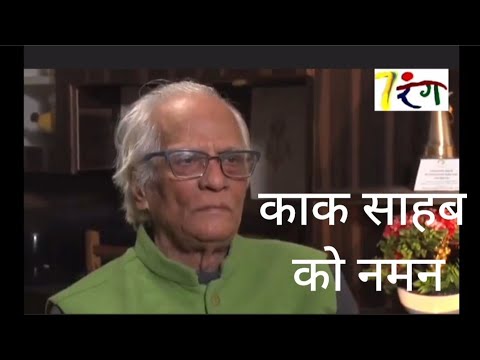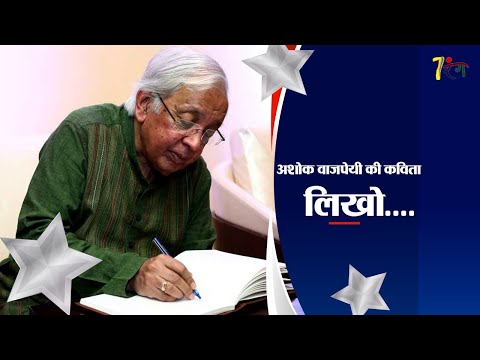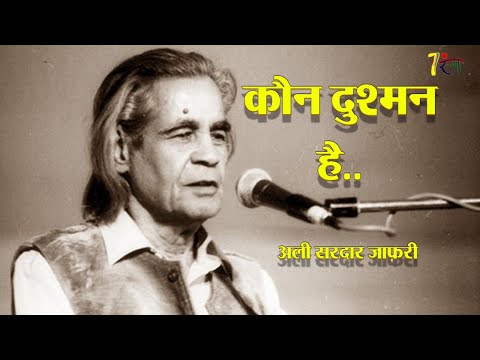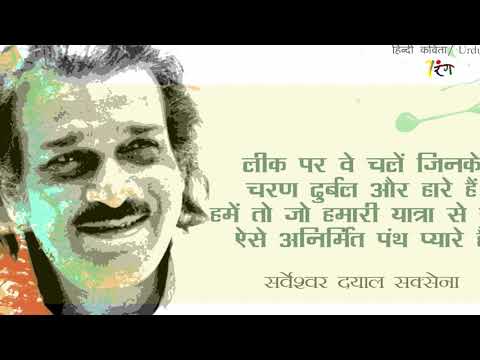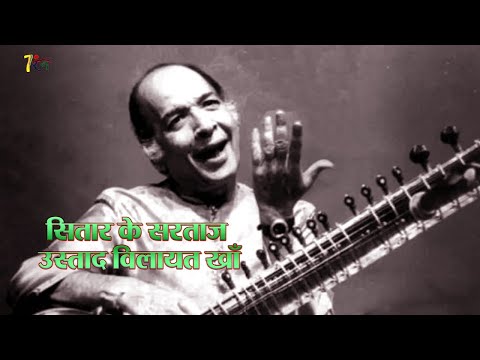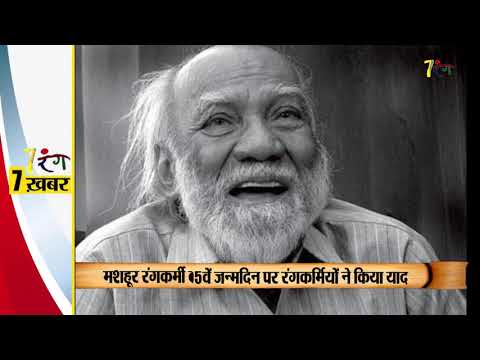- रवीन्द्र त्रिपाठी

क्या किसी कवि या लेखक को समझने के लिए उसकी कोई एक रचना कुंजी हो सकती है? ऐसी कुंजी जिसके माध्यम से हम उसके रचनालोक का प्रवेश- द्वार खोलें और पा लें कि उसके यहां क्या क्या है । इस प्रश्न का उत्तर हां भी है और नहीं भी। ये संभाव्यता और असंभाव्यता- दोनों इसलिए होती हैं कि किसी बड़े रचनाकार को लेकर विपुल व्याख्याएं-संभावनाएं होती हैं और उसे कैसे पढ़ा या समझा जाए इसे लेकर कोई सर्वमान्य और सार्वकालीन प्रविधि बनाना संभव नहीं है। जरूरी भी नहीं। फिर भी हर व्याख्या या दृष्टिकोण की अपनी वैधता होती है। साथ ही ये भी कि किसी रचनाकार या उसकी कृति/कृतियों को लेकर कई तरह की व्याख्याएं एक दूसरे को काटती या निरस्त नहीं करतीं। व्याख्या-संभावनाएं रचना या रचनाकार को विशिष्ट ही बनाती हैं। इसलिए कुंजी वाली बात से विष्णु खरे (9 फरवरी 1940- 19 सितंबर 2018) के काव्यकर्म को समझने का एक विनम्र, भले ही अपर्याप्त, प्रयास किया जा सकता है। खरे की एक कविता है –‘वाक्यपदीय’। ये बहुत बड़ी नहीं है। सिर्फ़ दो पृष्ठों में समायी है। पर खरे की सृजन-चेतना के व्याकरण को समझने में मदद करती है। कविता इस तरह शुरू होती है-
वह एक वाक्य बोलना चाहता था
जिसके प्रत्यय और अव्यय इस धरती से उठें
इसके सारे आवरणों से गुजरते हुए
चंद्रमा से टकराएं
सूर्य तक परावर्तित होकर उसकी प्रदक्षिणा करती शेष संतति तक छिटकें
उनसे होते हुए पार कर जाएं नीहारिकाएं श्वेत वामन कृष्ण विवर
और वे सारी दुनियाएं जो हुई थीं औऱ बनेंगीं
जाहिर है ये कोई साधारण वाक्य नहीं होगा। ये तो अनंतता की अग्रसर एक ऐसा वाक्य होगा जिसकी व्याप्ति मौजूदा दुनिया से परे भी हो। और ऐसा वाक्य तो किसी कवि की एक रचना भऱ नहीं होगी बल्कि उसकी संपूर्ण रचनाएं होंगी। क्या ये कहा जा सकता है कि किसी कवि की संपूर्ण रचनाएं एक लंबे वाक्य की तरह है? शायद ये विष्णु खरे के बारे में कहा जा सकता है क्योंकि `वाक्यपदीय’ कविता के अगले अंश या अंशों को पढ़े तो समझ में आता है कि उनकी संपूर्ण काव्याकांक्षा क्या थी-
एक बहुत लंबा वाक्य होगा वह
और वह चाहता था कि केवल ब्रह्मांड को ही नहीं जोड़े
वह प्रत्येक जीवित और दिवंगत के बीच से भी गुजरे
उसके कुछ अंश मृदु हों और कुछ कठोर
कुछ में संगीत हो और कुछ सुने न जा सकें
कुछ में प्रेम की कामनाएं हों सौहार्द्र रहे
कुछ हिस्सों में घृणा हो शत्रुता और संतृप्ति
मानवीय और अमानुष का समास हो उसमें
कुछ अंशों में अर्थ हो कुछ नितांत अर्थातीत
स्पष्ट है कि कवि ऐसी कविताएं लिखना चाहता है जिसमें कई तरह के तजुर्बे, जजबात और विचार मौजूद हों। और तजुर्बों और जजबात से परे भी कुछ बातें हों। और जरूरी नहीं कि वे सब एक दूसरे की सहयोगी या पूरक ही हों बल्कि परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। असंबद्ध भी। पर, कवि की चाहत है कि, ये सब एक ही सृजन- इच्छा के तहत हों या ऐसी समझी जाएं। दूसरे शब्दों में कहें तो हर कविता एक वाक्यांश हो और वाक्य अनंनता की संभावना से युक्त हों ।

इसीलिए विष्णु खरे के कवि-व्यक्तित्व को किसी एक खांचे या सांचे में ढाला नहीं जा सकता। उनके यहां भिन्न प्रकार की कविताएं हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि जिनका भरपूर आस्वाद करने के लिए पाठक को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। कई बार शब्दों के अर्थों के लिए शब्दकोष देखने पड़ सकते हैं क्योंकि उर्दू की ऐसी शब्दसंपदा उनके यहां है जो आम बोलचाल में नहीं मिलती। और हां, आवश्यक नहीं कि शब्दकोश से ही काम चल जाए, आपको विश्वकोश यानी इनसाइक्लोपीडिया भी देखना-पढ़ना पड़ सकता है अरबी या फारसी साहित्य के किस प्रसंग का उल्लेख किया जा रहा है। ये कवि काव्य-रसिकों की कड़ी परीक्षा भी लेता है। खरे की कविता का संपूर्ण रस लेने के लिए कई तरह के स्रोतों की मदद लेनी पड़ती है। गजानन माधुव मुक्तिबोध की भाषा में कहें तो पाठक को `ज्ञानात्मक संवेदना’ की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जितना अधिक ज्ञान का विस्तार होगा उसी अनुपात में कविता का मर्म उद्घाटित होगा। यही नहीं, बाज दफे खरे की वाक्य-रचना भी ऐसी हो जाती है कि ठहरकर सोचना पड़ता है कविता या पंक्ति का तात्पर्य क्या है। उनकी कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जिसे पढ़ने के लिए वो अध्ययन-कौशल चाहिए जो किसी नृतत्वशास्त्रीय या समाजशास्त्रीय अध्येता के पास होती है और जो किसी सामाजिक परिघटना को समझने या जानने के लिए छोटे से छोटे तथ्य का भी संज्ञान लेता है और फिर उसे अपने आख्यान में समेटता है। `सिर पर मैला ढोने की अमानवीय प्रथा’ `हर शहर में एक बदनाम औरत होती है’, `जिनकी अपनी कोई दुकान नहीं होती’ जैसी कविताएं कुछ सामाजिक प्रक्रियाओ के रेशे रेशे को उघाड़ती है। इनको पढ़ना सिर्फ कविता पढ़ना नहीं रह जाता बल्कि अपने आसपास के परिवेश और सामूहिक मानसिक बनावट को बारीकी के स्तर पर जानना भी हो जाता है। हमारे दैनिक जीवन में भाषा के स्तर पर, तर्क और सोच के स्तर पर, विद्वेष और पूर्वग्रह की कई धारणाएं मौजूद होती हैं और इनके प्रति हम सजग नहीं होते। ये सब समाज के बड़े वर्ग में इस तरह रच बस जाती हैं कि लोग ये भी महसूस नहीं कर पाते कि अमुक धारणा किसी दूसरे (व्यक्ति या समुदाय) के व्यक्तित्व का अवमूल्यन कर रही हैं और इस प्रक्रिया में धारणा बनाने वालों के भीतरी वजूद को भी विरूपित कर रही हैं। खरे की कुछ कविताओं को पढ़ना सामूहिक चित्त के उस गह्वर में प्रवेश करना भी है जहां भांति भांति के पूर्वग्रह साथ मिलबैठकर हंसी ठट्ठा कर रहे होते हैं और किसी कमजोर या वेध्य का मजाक उड़ा रहे होते हैं। `हर शहर में एक बदनाम औरत होती है’ किसी बदनाम औरत को लेकर नहीं बल्कि समाज में व्याप्त औरतद्वेषी दृष्टिकोण को दिखाती हैं-
वह एक ऐसा वृतांत ऐसी किंवदंति होती है
जिसे एक समूचा शहर गढ़ता और संशोधित-संवर्धित करता चलता है
सब आधिकारिक रूप से जानते हैं कि वह किस-किस से लगी थी
या किस- किस को उसने फांसा था
सबको पता रहता है कि इन दिनों कौन लोग उसे चला रहे हैं
कई तो अगल-देखकर शनाख्त कर डालते हैं
कि देखो-देखो ये ये उसे निपटा चुके हैं
उन उनकी उतरन और जूठन है वह
स्वाभाविक है कि यह जानकारियां सबसे ज्यादा और प्राणाणिक
उन दुनियादार अधेड़ और बुजुर्ग गृहस्थों के पास होती है
जो बाकी सब युवतियों स्त्रियों को साधिकार बिटिया बहन भाभी कहते है
भारत के हर शहर, कस्बे और गांव में औरतों को लेकर ऐसी किंवदंतिया बनाई और पाई जाती हैं। इन सबको महसूस करने के लिए समाजशास्त्रीय (या नृतत्वशास्त्रीय) निगाह चाहिए जो खरे के पास है। सिर्फ इसी कविता में नहीं कुछ अन्य कविताओं में भी वो निगाह दिखती है।

विष्णु खरे एक बड़े कवि, उत्कृष्ट अनुवादक, हिंदी और विश्व-सिनेमा के गंभीर अध्येता, तीखे तेवर वाले साहित्य समीक्षक, भारतीय और पश्चिनी संगीत के रसिक और निर्भीक पत्रकार थे। हिंदी की दुनिया उनको इन सभी रूपों मे याद रखेगी। मानवीय रिश्तों के प्रति गहरा लगाव रखनेवाले खरे आपसी रिश्तों की परवाह किए बिना जरूरत पड़ने पर खरी खरी कहने और लिखने में विश्वास करते थे। यहां ये भी कहना जरूरी है कि खरे का बौद्धिक पक्ष `पोलेमिक्स से निर्मित था। निजी जीवन में भी और आलोचनात्मक लेखन में भी वे उन बुद्धिजीवियों, आलोचकों और कवि-कथाकारों पर बोलते और लिखते रहते थे जिनसे वे असहमत होते थे। उनमें अतिरंजनाएं भी थीं और कुछ लोगों के लिए उनकी कलम परशुरामी फरसे की तरह हो जाती थी। कभी कभी तो क्रोध भी परशुरामी ही जाता था। उनके भीतर आक्रोश की धारा निरंतर बहती रहती थी। इसका एहसास भी उनको था।उनकी कविता `करना पड़ता है’ शरू में ही आता है-
मेरी ख्याति कोई मिलनसार या परोपकारी आदमी की नहीं/ बल्कि मुझे बददिमाग और अमानवीय ही माना गया है
और इसी से जुड़ा पहलू ये भी हैं कि समकालीन हिंदी जगत में खरे जैसा कोई मूर्तिभंजक नहीं हुआ। और इसका विलोम भी इस मायने में सही है कि वे साहित्य संसार के एक बड़े मूर्तिकार भी थे। हिंदी कविता में कई युवा प्रतिभाओं को सामने लाने और उनको स्थापित करने के लिए रुचि दिखाने वाले भी उनके जैसे विरल लोग ही हैं। निजी स्तर पर वे कई परस्पर-विरोधिताओं के पुंज थे।
बतौर कवि विष्णु खरे ने न सिर्फ एक खास तरह की भाषा और संवेदना से समकालीन हिंदी कविता को नया मिजाज दिया बल्कि उसे बदला भी । एक बड़े कवि की पहचान इस बात से भी होती है कि वह पहले से चली आ रही कविता को कितना बदलता है। और इस लिहाज से खरे अपनी पीढ़ी और हमारे समय के एक बड़े उदाहरण हैं। `खुद अपनी आंख से’, `सबकी आवाज के पर्दे में’, `काल और अवधि के दरमियान’, `पिछला बाकी’, `पाठांतर’ `आलैन और अन्य कविताएं’ जैसे काव्य संग्रहों में उनका जो काव्य- व्यक्तित्व उभरता है उसकी मुकम्मल पहचान तो आनेवाले समय में होगी और लगातार होती रहेगी क्योंकि किसी बड़े कवि का आकलन कभी पूरा नहीं होता। वो तो सतत चलने वाला सिलसिला है। बदलते वक्त और नवीन विचारों और दृष्टिकोणों के आलोक में उसे हमेशा नए सिरे से जानने और पढ़ने की जरूरत बनी रहती है।
खरे का काव्य संसार कई प्रकार की आवाजों से भरपूर हैं। ये सभी आवाजें हमारे समय में भी मौजूद हैं और अनंनता में भी। पीड़ित मनुष्य की आवाजें भी उनके यहां हैं और पशुओं और जानवरों की आवाजें भी । उनकी कविताओं में चिड़ियों का गान भी है जो उनकी `सुंदरता जैसा ही सुंदर होता’ है, तोतो की `तीखी वास्तविकतावादी चीखें’ (शायद ही किसी कवि ने तोतों की आवाजों के बारे में इस तरह के विशेषण का प्रयोग किया हो) और अनोखी बोलियां भी हैं। उल्लू, कौवे, बंदर, बकरी भी उनकी कविताओं मे आते हैं और याद छोड़ जाते हैं। जो हैं. जो थे और जो भविष्य में होगें – सबको समेटने की चाहत है उनके यहां।
`लालटेन जलाना’ खरे की एक अविस्मरणीय कविता है। बहुचर्चित भी। और एक खास अर्थ में प्रतिनिधि भी। सामान्य जीवन में लालटेन जलाना एक मामूली-सी चीज़ मानी जाती है। पर खरे जिस ढंग से इस मामूली-सी चीज़ के विभिन्न पहलुओं को सामने लाते है उससे ये बात खुलती जाती है आम जीवन का सामान्य पक्ष तरह तरह की पेचीदगियों और सौंदर्य से भरा है। ये कविता लालटेन जलाने भर की नहीं रह जाती है बल्कि सामान्य जीवन के उलझावों और सुंदरताओं को दिखाने की कविता भी बन जाती है-
लालटेन जलाने की प्रक्रिया में लालटेन बुझाना
या कम करना भी शामिल है
जब तक विवशता ही न हो तब तक रोशनी बुझाना ठीक नहीं
लेकिन सोने से पहले बाती कम करनी पड़ती है
कुछ लोग उसे इतनी कम कर देते हैं
कि वह बुझ ही जाती है
या उसे एकदम हल्की नीली लौ तक ले जाते हैं
जिसका एक तरह का सौंदर्य निर्विवाद है
लेकिन लालटेन के हिलने से या हवा के हल्के से झोंके से भी
उसे बुझने का जोखिम है
लिहाजा अच्छे जलाने वाले
लालटेन को अपनी पहुंच के पास लेकिन वहां रखते हैं
जहां वह किसी से गिर या बुझ न जाए
और बाती को वहीं तक नीची करते हैं
जब तक उसकी लौ सुबह उगते सूरज की तरह
लाल और सुखद न दिखने लगे
लालटेन बिजली के इस दौर में छोटे शहरों में भी लुप्त होता जा रहा है और गावों में भी। पर अभी भी गांवों और कस्बों में लालटेन जलते हैं या जलाए जाते हैं। ये तो दैनिक जीवन का व्यावहारिक पक्ष है। हो सकता है कि भविष्य में लालटेन हमारे दैनिक जीवन से लगभग गायब हो जाए। तब इस कविता का क्या होगा? क्या ये तब भी पाठकों और काव्य- रसिकों को मुग्ध करती रहेगी? अवश्य, इसलिए कि साधारण समझे जाने वाले काम के दौरान कितनी सजगता और कितना सौंदर्यबोध मौजूद होना चाहिए – इसकी तरफ ये इशारा करती है। ये कविता एक रूपक हो जाती है जिसमें अतीत या वर्तमान के ही नहीं भविष्य के मानवकर्म के कई एहसास उपस्थित है। कवि या कलाकार का एक काम उन कार्यव्यापारों, वाकयों और दृश्यों को रेखांकित करना या सामने लाना भी है जिनसे हम रोजाना परिचय में होते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों को वो साधारण या नगण्य दीखते हैं। इतने कि ये जानने की कोशिश भी नहीं करते उनके भीतर कितने बारीक अवयव मौजूद हैं। खरे विवरणों के माध्यम से बारीकियों में जाते हैं। `लालटेन जलाना’ कविता पढ़ने के बाद आप लालटेन जलाने या बुझाने तक के तथ्य तक ही सीमित नहीं रह जाते अपितु रोजमर्रे की जिंदगी को नए तरीके से महसूस करना शुरू कर देते हैं। कविता के मर्म का दायरा फैलता जाता है और नई कल्पनाएं उपजने लगती हैं। घरों से लेकर सड़क तक झाडु लगानेवाले (या लगानेवालियां), गैरोजों में कार या किसी अन्य वाहन की सफाई करनेवाले (या करनेवालियां), जैसों के अत्यंत साधारण कहे जानेवाले के कामों के साथ एक तादाम्य होने लगता है और पाठक के भीतर से आवाज आने लगती है कि इनके कामों और उनके भीतर निहित सूक्ष्मताओं को देखो। लालटेन जलाना ऐसी क्रिया हो जाती है जिसकी जद में दूसरी क्रियाएं आने लगती हैं। अपने आप। यानी इसके लिए कवि अपनी तरफ से कोई सायास संकेत नहीं देता।
गरीब, वंचित या निर्धनों के प्रति लगाव से तो साहित्य या कविता बहुत पहले से जुड़ चुकी है। किंतु खरे की कविता में सिर्फ ये लगाव भर नहीं है। वे यहां भी कई तरह के `केस स्टडी’ करते हैं। `देर से आनेवाले लोग’ कविता में वे एक ढाबे में खाना खाने आनेवाले की आदतों और मनोभावनाओं को सामने लाते हुए ढाबे में होनेवाले उन वाकयों की तरफ भी हमारा ध्यान दिलाते हैं जो हिंदी कविता में नहीं आई हैं-
उन्होंने कई बार आलुओं से माचिस की तीलियों को
और थालियों के किनारे चिपकी हुई
सूखी दाल सरीखी किसी चीज को निकाला है
बर्तन वाले को वहीं पेशाब के लिए झुकते
और बड़े रसोइए को उस नेपाली लड़के की गोद में बैठाकर
प्यार करने की कोशिश करते हुए देखा है
किंतु ये सभी जानते हैं
ढाबे में देर से आने वाले लोग कुछ नहीं कहते हैं
कौन होते हैं ढाबों में देर से आनेवाले लोग? ये सामान्य निम्न या उच्च मध्यवर्गीय परिवारों के तो नहीं होते। ये तो दिन भर की दिहाड़ी के बाद काम से मुक्त हुए लोग होते हैं जो किसी शहर में प्रवासी की हैसियत से होते हैं और परिवार के साथ नहीं रहते। किसी दूरस्थ इलाकों से काम और रोजगार के लिए आए हुए लोग। ऐसे लोग एक ही कमरे में चार-पांच या और भी अधिक समूहों में साथ रहते हैं। कविता पढ़ने के बाद ऐसे लोगों को लेकर मन में और भी खयाल आते हैं और इन खयालों का सिलसिला बढ़ता जाता है। इस तरह ये कविता पूरी होने के बाद खत्म नहीं होती। वो पाठक के मन में और भी विस्तारित होती रहती है और अनंनता की ओर बढ़ते वाक्य मे तब्दील हो जाती हैं।
।
खरे ने हिंदी कविता के अंत: करण को काफी बदला। ये बदलाव किस तरह का था? कई बातें कही जा सकती है कि पर पहली तो यही कि वे हिंदी कविता को गद्य के काफी करीब ले गए। हालांकि इसकी शुरुआत तो मुक्तिबोध से हो चुकी थी। खरे उसे और आगे ले गए। उनकी कविता में गीतात्मकता या `लिरिसिज्म’ नहीं के बराबर है। उनकी ज्यादातर कविताएं या तो निबंधों या लेखों की तरह हैं या आख्यान/कहानी के साचें में ढली हई। खरे एक पत्रकार रहे और पत्रकारिता में भी उनका इलाका मुख्य रूप से संपादकीय या अग्रलेख-लेखन का था (फिल्म समीक्षाओं को छोड़ दें तो।) जैसा कि संपादकीयों या अग्रलेखों में होता है – किसी खास विषय पर विचार और विश्लेषण किया जाता है, उसके अलग अलग कोण देखे या दिखाए जाते हैं और कुछ परिकल्पनाएं की जाती हैं। यह पद्धति खरे की कई कविताओं मे मौजूद है।
यहीं पर, ठहरकर, ये भी कहा जाना चाहिए कि गद्य या गद्यात्मकता का कोई एक निश्चित ढांचा नहीं होता है। जैसे कई तरह की काव्यात्मकता या पद्यात्मकता होती है वैसे ही विभिन्न किस्म की गद्यात्मकता होती है। खरे की कविताओं के भीतर की कई शैलियों की गद्यात्मकताएं है। और इनमें एक है- गद्य- कविताएं। उन्होंने अच्छी संख्या में गद्य- कविताएं भी लिखी हैं। हिंदी में उनके पहले त्रिलोचन शास्त्री, रघुवीर सहाय और उनके लगभग समकालीन मंगलेश डबराल के भी इस विधा में लिखा है। ख़ैर, उनको फिलहाल छोड़ दें और खरे तक ही सीमित रहे तो इस काव्य-विधा या उप-विधा के माध्यम से भी उन्होंने बारीक एहसासों को हिंदी के काव्य-जगत में लाया जो आधुनिक दौर में भी अकाव्यात्मक मानी जाती रही। जैसे `प्रतिसंसार’ कविता को ही लीजिए जो फोटोस्टेट कराने को लेकर है। आजकल बहुत सारे लोग, खासकर शोधार्थी और छात्र पुस्तकालयों या दुकानों में किताबों, पत्रिकाओं या उनके कुछ अंशों के फोटोस्टेट कराए पाते जाते हैं। फोटोस्टेटीकरण के उस दौरान भी फोटोस्टेट करानेवाले और करनेवाले के मन के भीतर कुछ कुछ होता रहता है। ये क्षणभंगुर किस्म की मन:स्थितियां होती है जिसे काव्य की परिधि में लाने का खयाल बहुतों को फालतू का या मह्त्वहीन लग सकता। मगर खरे के लिए वो मह्त्तपूर्ण है – `इन प्रतिलिपियों से एक विचित्र, विविध प्रकीर्णिका बनती रहती है एक अनपढ़े अनकिए का पुस्तकालय तैयार होता जाता है कितने लोग कितने विचार कितना सृंजन एक समानांतर संक्षिप्तिकृत संचयित प्रतिसंसार उसके यहां बढ़ता जाता है…।
इस कविता में और ऐसी अन्य गद्य कविताओं में कोई अल्पविराम, अर्धविराम या पूर्णविराम नहीं होता। (हालांकि खरे की दूसरी कविताओं में भी किसी तरह के विराम चिन्ह नहीं होते लेकिन अलग पंक्ति का भान बना रहता है लेकिन गद्य कविताओ मे वो भी नहीं होता।) इस आधार पर भी कह सकते हैं कि `प्रतिसंसार’ या कवि दूसरी गद्य- कविताएं भी अनंनता की ओर अग्रसर वाक्य हैं जिसे पाठक अपनी तरफ से, कम से कम, अपने मन में बढ़ा भी सकता है।ये गद्य कविताएं अपने में अपूर्ण भी है किसी संपूर्णता की तऱफ बढ़ती हुई भीं।
जहां तक आख्यानों/ कहानियों (या नैरेटिव) के शिल्प का प्रभाव है इस सिलसिले में उनकी कुछ कविताएं यहां याद की जा सकती हैं। `गुंग महल’,` होनहार’ `न हन्यते’ जैसी कविताएं इसी तरह की है। फिलहाल एक को ही लें यानी `न हन्यते’ को। शीर्षक गीता के दूसरे अध्याय के बीसवें श्लोक की एक उक्ति की याद दिला देता है –`न हन्यते हन्यमाने शरीरे’। यानी शरीर के मरने पर भी आत्मा अमर रहता है। लेकिन कविता ये नहीं दुहराती। वह गीता की इस उक्ति से अलग दिशा में जाकर विडंबनापूर्ण तरीके से ये कहती है कि कई लोग हत्याएं करते हैं और उनको अपना शौर्य समझते हैं।
लेकिन उनके भीतर किसी तरह का अपराध- बोध नहीं होता। उनको एक स्तर पर तो लगता है कि वे कुछ गलत कर रहे हैं इसलिए ऐसा करते हुए घिन भी आती है फिर भी इसे सामाजिक कर्तव्य समझते हैं। लेकिन वे जीवन भर समझ नहीं पाते कि उन्होंने कोई गलत या आपराधिक काम किया था। `न हन्यते’ कविता उस आदमी की तरफ से एक बयान है जो एक वक्त पहलवानी करता रहा और जिसने भारत की आजादी और विभाजन के दौरान उपजी हिंसा के दौर में अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ निरीह मुसलमानों की हत्या की थी। बिलकुल सहज तरीके से, हालांकि कुछ कुछ लज्जाशीलता के साथ, वह अपने कारनामें बताता है-
रात से लेकर मुंह अंधेरे तक कभी इस किनारे बैठ जाते कभी उस
इक्कों और तांगों को नहीं छेड़ते थे
पर पैदलों और साइकिलवालों को सलाम या आदाबर्ज वगैरह कहकर रोक लेते
पहचानने के और भी तरीके थे
अक्सर तो यही दर्जी नाई भिश्ती जुलाहे तरखान मिस्त्री झल्लीवाले होते थे
कुछ तो पता नहीं कैसे हमें पहचान जाते थे
पंडज्जी लालाजी ठाकुर साहब कहकर पैरों पर गिरने लगते थे
ऐसों को तो छोड़ ही नहीं सकते थे
सो काम खत्म किया वही बोरे ऱखते थे उन्हीं में डाला
रस्सी में बांधा और नीचे जमनाजी में घसीटकर बहा दिया
क्रिशन भगवान ने गीता मे कहा है कि पापियों को मारने से पाप नहीं लगता
फिर भी छीना-झपटी से इतनी घिन हो जाती थी
कि जमनाजी में अस्नान कर निगमबोध के हनुमानजी के सिर नवा
कौड़िया पुल के पास गरम दूध पीकर ही लौटते थे
आखिर इस तरह की `आपराधिक कर्तव्यबोध’ क्यों आ जाता है कुछ लोगों में? और क्या कुछ गिने चुने लोगों में आता है या समाज का एक बड़ा वर्ग इस तरह की `कर्तव्यबोध’ को अपनी `सामाजिक जिम्मेदारी’ मान लेता है और अपने किए को `शौर्य’ समझता है? अपने इस `शौर्य’ के किस्से आगे चलकर अपने परिचितों और भावी पीढ़ियों को सुनाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसी अपराधबोधहीनता सिर्फ भारत- पाकिस्तान विभाजन के दौर को लेकर ही हो। दिल्ली में सिख-विरोधी दंगे या गुजरात में गोधरा-हादसे के बाद सामूहिक नरसंहार के बाद भी ये सब चलता रहा। ये पूर्व यूगोस्लाविया के विघटन बाद सर्बिया, क्रोएशिया या बोस्निया हरजेगोविना में भी यही होता रहा। ये एक विश्वव्यापी व्याधि है। ऐसी मानसिक बीमारी जो व्यक्ति को उस संवेदनशालला से हीन कर देती है जो हर मनुष्य में होनी चाहिए। कई बार तो कुछ लोग `हमनें इतने को मारे’ का `गौरवबोध’ लेकर जीते रहते हैं। क्या इस तरह का `गौरव बोध’ इसलिए नहीं पैदा होता कि हममें से कुछ या कई `दूसरा’ गढ़ लेते है। ये `दूसरा’ किसी खास धर्म का हो सकता है या किसी खास जाति या राष्ट्रीयता या समुदाय का। उस `दूसरे’ को सबक सिखाना या उसे नेस्तनाबूद करना `पुनीत कर्तव्य’ मान लिया जाता है।
भारत विभाजन के समय बड़े पैमाने पर हत्याएं हुईं। बलात्कार किए गए और स्त्रियों के शीलहरण हुए। सआदत हसन मंटो की कई कहानियां इसका साक्ष्य हैं। हिंदी में य़शपाल से लेकर भीष्म साहनी तक की कथा-रचनाओं में भी उस हिंसा के कई रूप आए हैं। अभी भी इतिहासकारों और समाजविज्ञानियों में शोध और चिंतन चल रहे हैं कि सामूहिक हिंसा के उस दौर की व्याख्या किस तरह की जाए। `न हन्यते’ ऐसे शोधार्थियों और व्याख्याकारों के सामने नई खिड़की खोलती है कि इस आलोक में भी सामूहिक हत्या को देखा जा सकता है। `न हन्यते’ एक वातायन है, उस हिंसक दौर और उसमें शामिल लोगों की मन:स्थितियों को समझने का जो उसमें शामिल रहे हैं जो आज उसे याद करते हुए, सकुचाते हुए भी, अपने किए को राष्ट्र/समुदाय के लिए किया गया वीरोचित कर्म मानते हैं।
विष्णु खरे की एक बड़ी ताकत अमूर्त से एहसासों को ठोस और सघन बनाना है। इसी को लक्षित करते हुए वरिष्ठ कवि मंगलेश डबराल ने लिखा है- `वे कोमलता और आत्मीयता के बारीक स्वरों को छेडते रहते हैं और उन अनुभवों को भी, जो अकसर खामोश, अस्पष्ट, धुंधले और अमूर्त रहते हैं, जिन्हें एहसासों और सिहरनों के अलावा कोई भाषा दे पाना कठिन होता है’। ये तो माना ही जाता है कि संगीत एक सर्वाधिक अमूर्त कला है। और संगीत सुनने का अनुभव? वो तो और भी अमूर्त हो गया। क्या उसे हम अलौकिक आदि विशेषणों से नहीं नवाजते। यानी एक ऐसा अनुभव जिस शब्दों में बयां करना नितांत कठिन बल्कि असंभव-सा है। लेकिन खरे इसे संभव बना देते हैं और संगीत सुनने से श्रोता और रसिक के भीतर क्या-क्या होता है, यानी उसके भीतर कौन- कौन-सी तब्दीलियां आती हैं, इसको अपने तरीके से बता देते हैं। `प्रवाह’ कविता को या उसके इन काव्यांशों को पढ़ने के बाद अचानक ही संगीत सुनने या सहृदय होने के मायने साफ साफ खुलने लगते हैं। –
यदि संगीत सुनना ही है
तो इस तरह कि धीरे धीरे लगे
तुम ही वह गायक या वादक होते जा रहे हो
और उससे आगे तुम ही वह संगीत
फिर तमाम सुननेवालों के बीच तुम अदृश्य हो जाओगे
क्योंकि तुम ही सभी सुननेवाले बन चुके होगे
क्योंकि वे भी अंतर्धान हो गए हैं
और आगार में एक नीरवता छा जायेगी
होते हुए भी अच्छा संगीत एक सन्नाटा फैला देता है
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
और कोई नहीं चाहेगा चाहेगा यह खत्म हो
फिर भी वह ख़त्म होगा
सब लौटेंगे वही बनने के लिए जो वे इससे पहले थे
लेकिन ठीक वैसे नहीं
उन्होंने जान लिया है
कि क्या होता है एक प्रवाह में बदलते बहते हुए सुर होना
और अब भले ही वे अलग हो गए हों
औऱ अब सब थोड़े थोड़े बज गूंज या संचालित हो रहे हैं एक दूसरे में
वे लीन हो रहे थे परस्पर लेकिन वह मृत्यु न थी
एक तरह का सतत पुनर्जन्म था जीते-जी
एक साथ कई रूपों मनोलोकों में
क्या कविता भी फिल्म की तरह लिखी जा सकती है? या क्या कविता को पढ़ने के दौरान भी फिल्म देखने का अनुभव हो सकता है? इन दोनों सवालों का उत्तर है- हां। और ये उत्तर खरे की कविता `1946 की एक रात’ देती है। वैसे तो ये कविता विष्णु खरे ने अपनी मां की मृत्यु को लेकर लिखी है जिनका निधन एक बीमारी के बाद 1946 में हो गया था। मां की मृत्यु के समय खरे की उम्र छह साल की थी। कविता बहुत बाद में लिखी गई। भावना के स्तर पर ये बेहद विचलित कर देने वाली रचना है। पर सिर्फ यही इसकी खासियत नही है। इसका जो बड़ा गुण है वो ये कि ये एक फिल्म की तरह है। यानी उसे पढ़ते हुए ये महसूस होता है कि आपके सामने एक फिल्म चल रही है जिसमें कैमरा एक घर की निविड़ रात्रि में मौजूद अंधकार और झीने प्रकाश को भी पकड़ रहा है। एक नारी चरित्र है जो अपनी आसन्न मृत्यु को आते देखते हुए अपने पति, अपने तीन बेटों और अपनी दो ननदों से मूक संवाद करती है और इसी क्रम में अपनी हसरतों को भी अमूक व्यक्त करती है। ये पुराने वक्त के मूल फिल्मों की तरह है। हिंदी में बहुत कम ऐसी कविताएं है जो फिल्मों की तरह लिखी गई है- यानी हर शॉट का ध्यान रखा गया है और साथ ही समग्र प्रभाव और अन्विति का भी-
घर में अंधेरा रहा होगा
लेकिन बाहर का कुछ- न-कुछ उजाला अंदर आ ही जाता है
उसके और दीवार के सहारे
वह किसी तरह उस दरवाज़े तक पहुंची होगा
जहां से परछी में सोया उसका पति दिखा होगा
जिसकी आधी तनख़्वाह उसके इलाज में जाती थी
और कोई मौका होता तो वह
उसके पैताने पहुंच उसके पांव छू लेती
जो जब उससे स्नेह जताना चाहता था तब उसे भालूजी कहता था
लेकिन इस वेला में
उसने यहां से प्रणाम कर लेना उचित समझा होगा
शायद उसने उससे माफ़ी मांगी हो कि उसकी सेवा न कर सकी
पलटकर उसने देखा होगा अंदर के कमरे में ज़मीन पर सोई
अपने से छोटी अपनी दोनों कुंआरी ननदों को
जो उसे लाख मना करने पर भी
उसकी तीमारदारी का रोग पाले हुए थीं
भाभियां ननदों के पैर छूती हैं
उसने भी मन ही मन किया होगा
उनके ब्याह की बाल-बच्चों की मानता की होगी
सोचा होगा भांवरो पर उसकी कौन-सी साड़ी
बड़ी बाई पर अच्छी लगेगी कौन-सी छोटी पर
खरे सिर्फ इस कविता में ही नहीं कुछ अन्य कविताओं में भी आत्मकथात्मक रहे। यानी उनकी जाती जिंदगी की स्मृतियां और घटनाएं उनपर छायी रही। `जैसे चौथे भाई के बारे में’ में वे अजन्मे या मृत (ये उनको भी मालूम नहीं था कि सच में क्या हुआ था) भाई (या बहन भी हो सकती थी) को लेकर सोचते हैं और कुछ खयालें उनके अंदर जन्म लेती हैं। `किसलिए’ कविता में भी वे अपने पिता, मां, बुआओं, भाइयों और खुद के बचपन की रेलयात्रा के प्रसंग के बहाने सुखद स्मृतियों को दर्ज करते हैं।
ये भी मानव मन का एक स्वभाव है कि बचपन उस पर हावी रहता है। तिक्तता और मधुरता-दोनों के साथ। फ्रांसीसी उपन्यासकार बालजक की जीवनी लिखते हुए जर्मन कथाकार और जीवनीकार स्टीफन ज्वाइग (या स्वाइग) ने ये दर्ज किया है कि किस तरह बाल्यावस्था के कई संदर्भ उसकी (बालजक की) कई रचनाओं में आते हैं और इनको जान लेने से बालजक की रचनाओं का आस्वाद और गहर मे किया जा सकता है।
दरअसल खरे की रचनात्मकता की चार प्रमुख दिशाएं रही- पहली दिशा तो अपने परिवार और बचपन की ओर जाती थी, ; दूसरी आसपास व वर्तमान की जिंदगी के पर्यवेक्षण और विश्लेषण से संबंधित है और इसमें समसामयिक स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हैं। तीसरी दिशा अमूर्तनों को मूर्त करने की तरफ मुड़ी रहीं और चौथी इतिहास व मिथकों की ओर।
आइए इसी कड़ी में भारतीय मिथकों और पुराणकथाओं को लेकर उनके विमर्शात्मक रवैये को भी चिन्हित करें। महाभारत को आधार बनाकर उन्होनें कई कविताएं लिखी हैं। उनमें एक के बारे में यहां चर्चा करते हैं। कविता है `अग्निरथोSवाच’। अग्निरथ वह रथ है जिस पर महाभारत युद्ध के दौरान सारथि की भूमिका में कृष्ण बैठते थे और योद्धा के रूप में अर्जुन। कथा है कि युद्ध के बाद कृष्ण के उतरते और ध्वज पर से हनुमान के चले जाने के बाद वह रथ जल गया था। इस कविता में वही अग्निरथ अपनी बात कहता है जो बताता है कि पूरा युद्ध किस तरह अनैतिकताओं, फरेबों और धूर्तताओं से भरा था हालांकि लड़नेवाले उसे धर्मयुद्ध बता रहे थे-
क्या- क्या नहीं किया क्षेत्रज्ञ ने क्षेत्र में/भाइयों और स्वजनों के बीच रण हुआ सो हुआ/बूढ़ों को मारा गया गुरु हत्याएं हुईं/दबे स्वर में झूठ बोले गए कुश पर सब कुछ त्याग बैठे आसीनों को छला गया/जिसने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी उसने चक्र उठाया/भुजाएं काटी गईं नर-रक्त पिया गया/रथ से उतरे विपदाग्रस्त विनयी महारथी का शिरोच्छेद हुआ/जांघ पर गदा युद्ध मे किया गया प्रहार/ मरे हुए वीरों के मस्तक पर पैर रगड़े गए/नपुंसकों तक का वध हुआ
विष्णु खरे का जन्म मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुआ था। हालांकि वहां उनका पैतृक घर नहीं था पर ये छोटा-सा शहर उनकी काव्य- चेतना का अविभाज्य हिस्सा रहा। मुंबई और दिल्ली को छोड़ कर यहां यदा कदा लौटते भी थे। अपने जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने यहां किराए पर एक कमरा भी लिया था हालांकि मृत्यु के एक साल पहले उसे अस्वस्थता की वजह से छोड़ भी दिया था। छिंदवाड़ा के जन जीवन को लेकर उनकी कुछ यादगार कविताएं भी हैं। उनकी कविता मे कस्बाई जीवन के बहुतेरे चित्र हैं जो शायद छिंदवाड़ा से उसके नाभिनाल के रिश्ते के कारण ही हैं। यानी उनकी कविता में गहरी स्थानीयता है। पर वे सिर्फ स्थानीयता के कवि नहीं है। वैश्विकता के भी हैं। इसका एक प्रमाण है उनकी कविता `आलैन’ जो उनके आखिरी संग्रह में शामिल है। ये कविता सीरियाई-कुर्द मूल के उस बच्चे पर है जो अपने माता-पिता के साथ सीरिया के निकलने के वक्त नौका दुर्घटना के कारण पानी में डूब कर मर गया था। `आलैन’ कविता विश्व स्तर पर निर्वासित-प्रवासी-शरणार्थी समस्या एक संवेदनात्मक आख्यान है।
खरे ने हिंदी सिनेमा और विश्व सिनेमा पर भी काफी लिखा है। हिंदी में भी और अंग्रजी में भी।हिंदी फिल्म संगीत के चलते फिरते विश्वकोष थे। किस फिल्म के कौन से गाने की धुन किस संगीतकार ने बनाई ये सब उनकी उंगलियों पर था।
अनुवाद एक बड़ा क्षेत्र है जहां खरे का योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने न सिर्फ विदेशी साहित्य-जर्मन, डच, फिनिश आदि – का हिंदी में बड़े पैमाने पर अनुवाद किया बल्कि आधुनिक हिंदी कविता के अनुवाद अंग्रेजी के साथ साथ जर्मन में भी किए। इस लिहाज से खरे एक सेतु थे भारत और पश्चिम के बीच। विदेशी भाषाओं हिंदी में अनुवाद करने वालों में और भी कई लोग हैं लेकिन हिंदी से अंग्रेजी और जर्मन में अनुवाद करने वाले बहुत कम। इस दृष्टिकोण से देखें तो खरे ने भारत और यूरोप के बीच एक नया सेतु बनाया जो अभी काफी दुबला पतला है। अनुवाद अपने में एक बड़ा काम है और अगर कोई दूसरी भाषा से अपनी भाषा में और साथ साथ अपनी भाषा से दूसरी भाषा या भाषाओं में अनुवाद करे तो सांस्कृतिक महत्त्व और बढ़ जाता है। खरे साहित्य के संसार में एक विश्व नागरिक थे और उनकी साहित्यिक नागरिकता कई भाषाओं में थी।
(साहित्यिक पत्रिका ‘साक्षात्कार’ से साभार)
Posted Date:August 6, 2019
4:43 pm