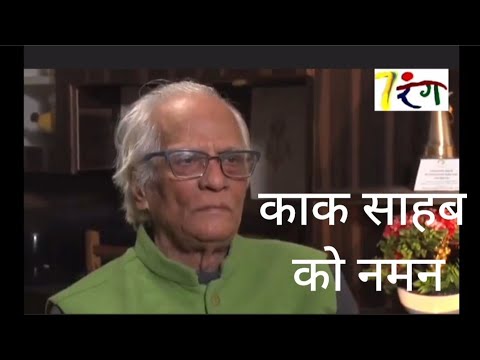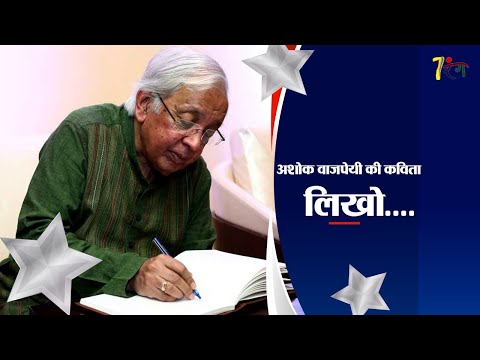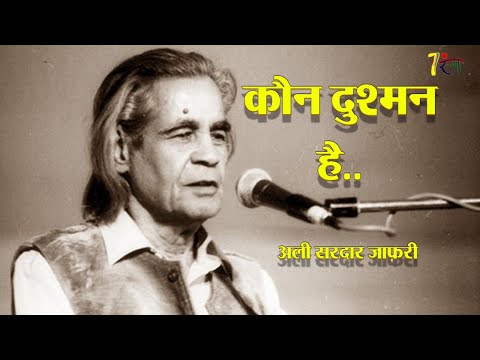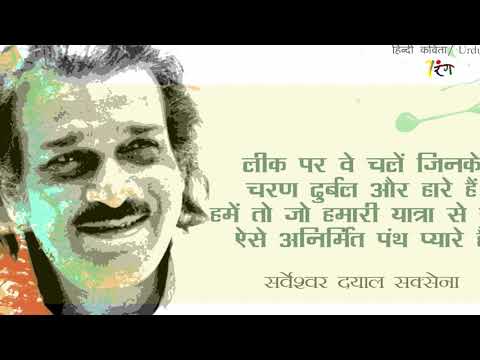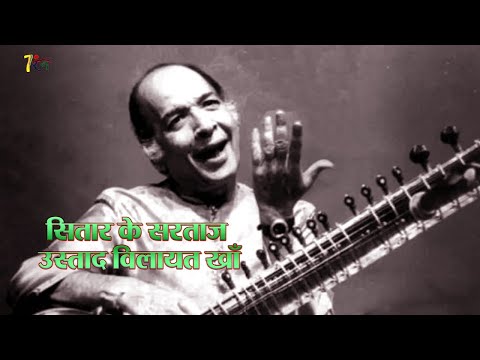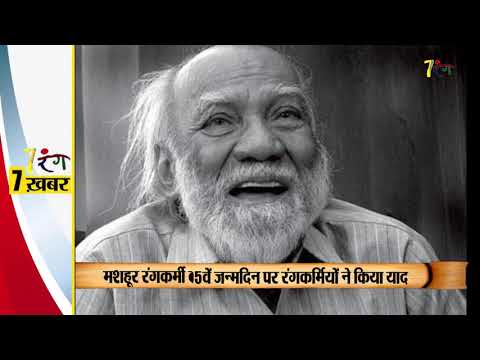यह कौन सा जल है जिसमें पांव डुबोती है संस्कृति?
जाने माने पत्रकार, लेखक और कवि प्रियदर्शन ने छठ पर्व को आज के संदर्भ में जोड़ते हुए इसके मर्म और सांस्कृतिक अवधारणा को बेहद खूबसूरती से शब्दों में ढाला है।
NDTV.IN पर छपा उनका आलेख पूरी मानवीय संवेदना के साथ धार्मिक कट्टरवाद और राजनीतिक भक्तों की क्रूरता को भी उठाता है और महानगरों में काम की तलाश में भटकते पूर्वांचलियों के दर्द को भी सामने लाता है… 7 रंग के पाठकों के लिए ये लेख साभार पेश है….
छठ की कई तरह की स्मृतियां मेरे भीतर हैं। दीपावली के बाद जब धूप नरम पत्तियों की तरह त्वचा को सहलाती थी और हवा की बढ़ती हल्की सी गुनगुनी ठंडक के बीच छठ की तैयारी शुरू होती थी तो उसमें सर्दियों के संकेत को हम पहली बार ठीक से पकड़ते थे। छठ की सुबह पहली बार हमारे स्वेटर निकलते थे। दिवाली में घर की सफाई के बाद झीलों, तालाबों और नदियों की सफ़ाई का सिलसिला शुरू होता और छठ के इस जल यज्ञ में हम डूबते हुए सूरज को भी शामिल कर लेते। एक मंद्र लय वाले उतार-चढ़ाव के बीच असंख्य कंठों से फूटते छठ के गीत पूजा को त्योहार में बदल देते थे।
यह सच है कि पूजा-पाठ के प्रति मेरे भीतर कभी आकर्षण नहीं रहा। ईश्वर के होने न होने की बहस निस्संदेह आकर्षक लगती रही और सूफ़ी परंपरा में अपने भीतर-बाहर ख़ुदा की तलाश करने वाले नग़मे भी एक तरह का भाव पैदा करते रहे, लेकिन बहुत सारे दबावों के बावजूद मन कभी इतना संस्कारशील नहीं हो पाया कि किसी पूजा-पाठ, मंत्रोच्चार में आस्था रख सके। उल्टे बाद के वर्षों में तरह-तरह के साहित्य के अध्ययन और धार्मिक संस्थाओं के पाखंड ने हर तरह के कर्मकांड के प्रति एक तरह की वितृष्णा पैदा की। आज के धार्मिक और राजनीतिक भक्तों की क्रूरता और उनका पाखंड देख यह वितृष्णा अपने चरम पर है।
इसके बावजूद होली के रंगों, दिवाली की रोशनी और छठ की छटा से जुड़ी बहुत सारी स्मृतियां ऐसी हैं जिनके कुछ मानवीय और सामाजिक पक्ष मुझे अब तक स्पंदित करते हैं। वैसे जिन दिनों की स्मृति की बात मैं कर रहा हूं, उन दिनों ऐसे टीवी चैनल नहीं थे जो पटना से पोर्टलैंड तक और दिल्ली से दुबई तक छठ के नज़ारे दिखाया करें, बल्कि ख़बरों का जो संस्कार था, वह छठ को किसी ख़बर की तरह नहीं, जीवन के एक अभ्यास की तरह देखता था।
आज जब तमाम चैनलों पर छठ के दृश्य देखता हूं, उससे जुड़े गीत सुनता हूं तो एक तरह ही कारुणिकता पैदा होती है। इस कारुणिकता में कुछ निजी तत्व भी है। क़रीब 28 बरस पहले रांची से दिल्ली आते हुए यह नहीं मालूम था कि मैं सिर्फ़ शहर नहीं बदल रहा हूं, बहुत सारा कुछ छोड़ भी रहा हूं जिसमें पर्वों की सामूहिकता भी है, छठ का उल्लास भी है।
लेकिन इस कारुणिकता का एक सामाजिक तत्व भी है। छठ धीरे-धीरे जैसे उजड़े हुए लोगों की स्मृति का भी त्योहार होता जा रहा है। दिल्ली और मुंबई से छठ से पहले जो ट्रेनें यूपी-बिहार की ओर चलती हैं, वे ऐसी ठसाठस भरी होती हैं कि उन्हें देखकर हैरानी होती है। जैसै सारा पूर्वांचल इसलिए अपने घरों की ओर चल पड़ा है कि किसी छूटे हुए तालाब, किसी छूटी हुई नदी, किसी छूटे हुए पोखर में एक शाम और सुबह अपने बिवाई लगे पांव डुबो सके, जैसे बरसों-बरस मिलने और सहेजे जाने वाले सारे ज़ख्म इस एक जल स्पर्श से ठीक हो जाएंगे। बरसों-बरस पराये महानगरों के सबसे ज़रूरी काम करने वाले और उनका पूरा बोझ उठाने वाले लहूलुहान कंधे और सिर छठ का दौरा उठा कर ही इतने हल्के हो जाएंगे कि अगले एक साल तक फिर किन्हीं अनजान जगहों पर खटने की ऊर्जा पैदा हो जाएगी। तो इस सारे उल्लास का एक सामाजिक मनोविज्ञान है जिसे महसूस करना बहुत मुश्किल नहीं है।
वैसे यह मज़दूरों और मजबूरों का ही नहीं, सांस्कृतिक रूप से अपनी धरती से उखड़ चुके उच्च मध्यवर्गीय खाते-पीते घरों का भी त्योहार है जो ट्रेन पकड़ कर आरा-पटना-गया नहीं लौटते, लेकिन दिल्ली, नोएडा या गाजियाबाद के नए इलाक़ों में बनती सोसाइटीज़ के स्विमिंग पूल से लेकर किसी छोटी सी झील में अपना यूपी-बिहार बसा लेते हैं। यह तादाद इतनी बड़ी है कि दिल्ली से मुंबई तक छठ मनाने या न मनाने पर राजनीति की जा सकती है।
लेकिन पूर्वांचल को इस तथ्य से कितना ख़ुश होना चाहिए। यह सच है कि देश ही दुनिया में भी इस पूर्वांचल ने- यूपी-बिहार के लोगों ने- अपने झंडे गाड़े हैं। लेकिन यह भी सच है कि यही पूर्वांचल तमाम जगहों पर अजनबी बना रहा है और अपने बाहरी होने की तोहमत भी सुनता रहा है, क़ीमत भी चुकाता रहा है। वह मुंबई में मार खाता है, असम में मार खाता है, श्रीनगर में मार खाता है, वह हर राजनीतिक टकराव का बहाना और निशाना बनता है। बिहारी होना गाली है, मूर्खता की निशानी है, पिछड़ेपन की पहचान है।
यह वह दुख है जो बिहार वालों को अब सालता नहीं। दिल्ली-एनसीआर में अब उनके इतने मकान हैं, यहां की भाषा में उनकी बोली इतनी घुल चुकी है कि वे शान से कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा यूपी-बिहार यहां वह है जो न वहां का है न यहां का है। उसे महानगर लॉकडाउन में रातों-रात दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल सकता है। उसे पैदल चल कर, साइकिल चला कर, उधार के पैसे से ट्रक-ऑटो कुछ भी करके- अपने छूटे हुए ठिकानों की ओर जाना पड़ता है- बस यह जानने के लिए कि सैकड़ों मील का सफऱ तय कर वह अपने जिस छूटे हुए घर में आया था, वह तो है ही नहीं, उस पर किसी और का क़ब्ज़ा है और वहां भी वह अनचाहा मेहमान है।
छठ दरअसल वह राहत है जो इन उजड़े हुए लोगों को उनका घर लौटाती है। विस्थापितों को भरोसा दिलाती है कि वे कहीं और स्थापित हो रहे हैं। उन्हें बताती है कि उनका एक पांव उस जल में है जो कहीं न कहीं किसी छोर पर उनके गांव की नदी में जा मिलता है।
इस लिहाज से यह धार्मिक पूजा-पाठ से ज़्यादा एक सामाजिक त्योहार बन जाता है। बेशक, हमारे इस सोशल मीडिया युग में सबकुछ विमर्श की वेदी पर चढ़ाया जाता है तो छठ के भी इससे अछूता रहने की कल्पना नहीं की जा सकती। यह पूछने वाले निकल सकते हैं कि प्रगतिशील तत्वों को छठ मनाने के कर्मकांड में क्यों पड़ना चाहिए और आधुनिक नारीवादी महिला को छठ का उपवास क्यों रखना चाहिए। लेकिन इस जड़विहीन समाज में सारे तर्क और विमर्श जैसे मनबहलाव के साधन हैं- वे अमूमन किसी सांस्कृतिक मूल्य के निर्माण की ज़रूरत से पैदा होते नहीं दिखते।
दिवाली और छठ फ़सलों की कटाई के बाद की समृद्धि के त्योहार हैं। दिवाली के साथ बहुत सारी भव्य और मिथकीय कहानियां जुड़ गई हैं, लेकिन छठ ने अपने-आपको ऐसी कथाओं से दूर रखा है। उसमें पंडित और उसका पतरा नहीं हैं, बस नदी का हिलता हुआ जल है, डूबते और निकलते सूर्यों की कांपती रोशनियां हैं, स्त्रियों का गीला आंचल है, उनके कंठ से फूटते गीत हैं, फल है और दौरा है और ठेकुआं है जिसमें स्वाद से ज़्यादा साझेदारी का सुख है। होली के अलावा यह दूसरा त्योहार है जिसने बाज़ार की दानवी जकड़ से खुद को बचाए रखा है। यहां ग़रीबी और सादगी भी किसी अभिमान की तरह खिलती है और घाटों पर सुबह-सुबह तिरते दीए किसी सभ्यता की उम्मीद की तरह दूर तक निकल जाते हैं।
तो छठ पर वाट्सैपीय बधाइयों, ठेकुआं, अर्घ्य की तस्वीरों तक सीमित न रहें, अपनी सांस्कृतिकता का मोल समझें और यह भी देखें कि अपने समाज से, अपनी जड़ों से कटी हुई, मूलत: राजनीतिक लक्ष्यों से प्रेरित तथाकथित धार्मिकता ने समाज में कितना ज़हर पैदा किया है। छठ का ठेकुआ यह ज़हर नहीं काट सकता, लेकिन यह दुख या संतोष बांट सकता है कि हममें से बहुत सारे लोगों को इस ज़हर की पहचान है।
(ndtv.in से साभार)
November 11, 2021
12:15 pm Tags: छठ, प्रियदर्शन, छठ और संस्कृति, पूर्वांचल और छठ, आस्था और छठ