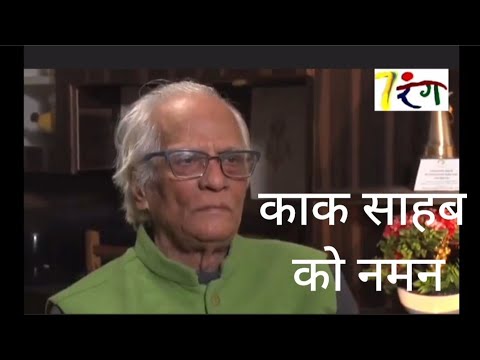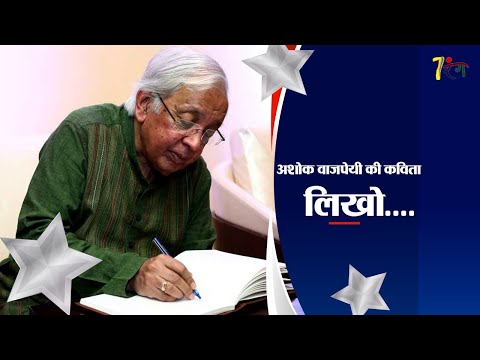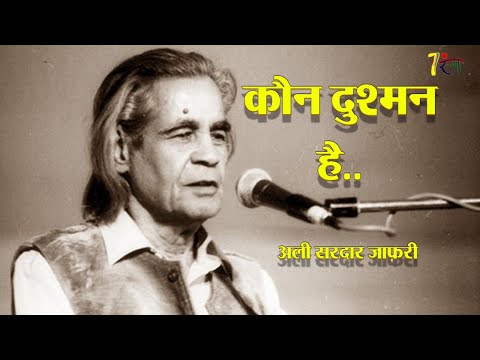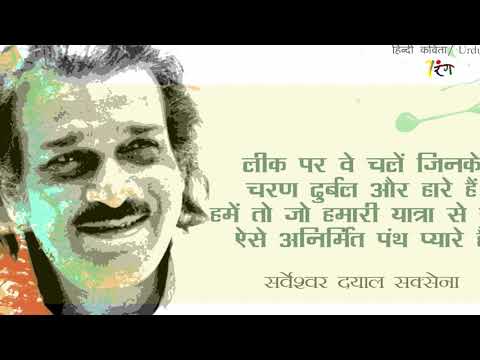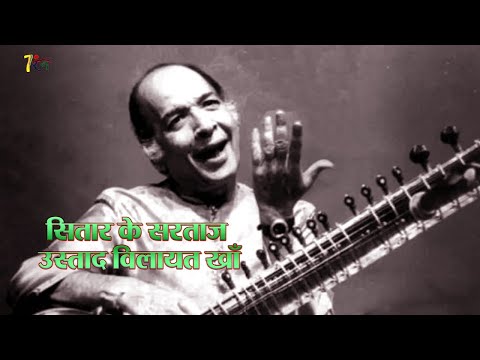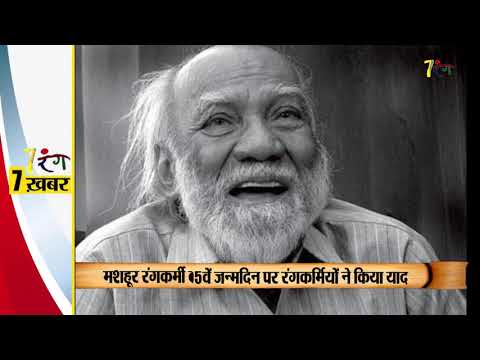क्यों विवादों में है ‘काशी का अस्सी’

दशाश्वमेध घाट और गंगा आरती के विहंगम और मनमोहक दृश्यों वाली काशी आखिर अचानक अपनी खालिस देसी गालियों के लिए खबरों में कैसे आ गई? दशाश्वमेध और अस्सी के बीच का फ़ासला बमुश्किल पांच किलोमीटर का होगा लेकिन यहां तक आते आते पूरी की पूरी संस्कृति आखिर कैसे बदल जाती है? गंगा भी वही है, गंदगी भी वैसी ही है लेकिन अल्हड़ और मस्त अंदाज़ के साथ साहित्य और संस्कृति का अनोखा मेल आखिर अस्सी पर ही क्यों दिखता है? जिन लोगों ने काशीनाथ सिंह को पढ़ा है और खासकर काशी का अस्सी के किरदारों को करीब से महसूस किया है वो इस हकीकत को समझ सकते हैं। डॉ चंद्रप्रकाश तो बहुत बाद में आते हैं, मोहल्ला अस्सी बहुत बाद में बनता है लेकिन अस्सी की सीढ़ियों पर मजमा बरसों से जमता आया है…। बनारस अपने तमाम रसों से सराबोर यहां हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागता है और हर शाम जवान होता है…साहित्य के लिए अस्सी से अच्छी जगह नहीं…। शायद इसलिए कि वहां तुलसी का अक्स दिखता है… संस्कृति के लिए अस्सी से बेहतर घाट नहीं.. शायद इसलिए कि वहां संगीत अपनी गहराइयों के साथ मन में उतर जाता है।

बनारस के घाट, काशी की संस्कृति और यहां का हर रंग ग्लैमर की दुनिया को हमेशा खींचता रहा है…। विदेशी पर्यटकों के साथ साथ हॉलीवुड भी यहां कैमरों और किरदारों के साथ मौजूद रहता है और बॉलीवुड की तो ये पसंदीदा नगरी है ही…अब सियासी मानचित्र में अहम मुकाम हासिल होने के बाद तो पूछिए मत…बनारस न तो बनारस रहा…काशी न तो काशी रही…बस खबरों की तिलस्मी नगरी बन गई…। काशी की काया पलटने के दावों के साथ मां गंगा के बुलावे पर आने वालों की धमक इतनी ज़रूर दिखती है कि अब अस्सी का सरकारीकरण हो गया है…। संस्कृति अब यहां हर सुबह अपने तमाम रंगों के साथ भैरवी गाती है…। बेहद सलीके से सांस्कृतिक विभाग का अमला यहां गंगा तट को सुरों के भिगो देता है…और ये एहसास दिलाता है कि अगर आपने अस्सी के सुबह-ए-बनारस को नहीं जिया तो कुछ नहीं किया…। गंगा तट पर सुबह के सूरज के साथ, आरती के दीपों के साथ संगीत के सुरों का आनंद नहीं लिया तो बनारस को महसूस नहीं किया। भले ही अब बनारस के लिए ये जुमला आम हो गया हो – सुबह-ए-बनारस, शाम बनारस…जब देखो तब जाम बनारस…।
लेकिन बनारस अपने जिस ताज़ा संस्करण के साथ चर्चा में है…। काशी की जो संस्कृति किताब से निकाल कर परदे पर उतारी गई है…। वहां चर्चा में बने रहने की एक कोशिश तो है ही…ज्यादा सहज और स्वाभाविक दिखने की चाहत में कला का बंटाढार भी है। काशीनाथ सिंह भले ही इससे खुश हो जाएं कि उनकी किताब पर डॉ चंद्रप्रकाश ने फिल्म बना दी और उनके पात्रों को हूबहू उतारने की कोशिश की.. लेकिन किताब पढ़ना और सिनेमा देखना दो अलग अलग चीज़ है…। जब आप साहित्य को सेलुलाइड पर उतारते हैं तो उसमें ज़रूरी बदलाव भी करते हैं, उसमें समसामियक पात्र और परिस्थितियां भी डालते हैं…लेकिन अपशब्दों की संस्कृति को परदे पर उतारकर आप किस अपसंस्कृति को बढ़ावा देते हैं, ये एक बहस का विषय है।
January 30, 2016
5:19 am